Attitude Meaning in Hindi: – अभिवृत्ति का अर्थ समझने के लिए हमे अपने रोजाना जीवन का अध्ययन ध्यानपूर्वक करना चाहिए क्योकि अभिवृत्ति/दृष्टिकोण को मनोवृत्ति ( Attitude ) के नाम से आजकल अधिक स्टूडेंट जानतें हैं
हाँ, इस सोशल मिडिया के जमाने में अक्सर स्टूडेंट एटीट्यूड किसे कहतें हैं? से अधिक एटीट्यूड इन हिंदी शायरी लिखकर गूगल में खोजतें हैं परन्तु मनोविज्ञान पढने वाला एक अच्छा और सच्चा छात्र हमेशा एटीट्यूड क्या होता हैं? का चुनाव करता है
एटीट्यूड विषय के इस लेख को थोडा अधिक ख़ास बनाने के लिए हम कुछ एटीट्यूड इन हिंदी शायरी के विषय पर अंत में यूनिक एटीट्यूड स्टेटस भी लिखकर देंगें जिससे हमारे उन यूजर का दिल न टूटें

जिनको अपने सोशल मीडिया पोस्ट के लिए एक अच्छा एटीट्यूड स्टेटस चाहिए लेकिन छात्रों के लिए यह जानना जरुरी हैं कि अक्सर एग्जाम में एटीट्यूड ( अभिवृत्ति/मनोवृत्ति ) को लेकर कुछ इस तरह प्रश्न पूछ लिए जातें हैं
- दृष्टिकोण किसे कहतें हैं?
- अभिवृत्ति क्या है? अभिवृत्ति के प्रकार सहित व्याख्या कीजिए?
- दृष्टिकोण का अर्थ उदाहरण सहित लिखिए?
- अभिवृत्ति के गुण और दोष बताइए?
- अभिवृत्ति का अर्थ और परिभाषा लिखिए?
इसीलिए हम सबसे पहले यह जानने का प्रयास करेंगे कि एटीट्यूड का मतलब क्या है हिंदी में?
Attitude Meaning in Hindi – Meaning of Attitude in Hindi – Attitudes Meaning in Hindi – मनोवृत्ति PDF.
मनोवृत्ति ( Attitude ) शब्द लैटिन भाषा के Aptus शब्द से लिया गया हैं जिसका अर्थ योग्यता या सुविधा होता है मनोवृत्ति/अभिवृत्ति का अर्थ रवैया या दृष्टिकोण होता हैं इसीलिए मनोवृत्ति को अभिवृत्ति या दृष्टिकोण भी कहा जाता है
मनोवृत्ति एक ऐसा शब्द है जिसका व्यवहार हम अपने दैनिक जीवन में दिन-प्रतिदिन करते है मनोवृत्ति किसी व्यक्ति की मानसिक तस्वीर या प्रतिच्छाया हैं जिसके आधार पर वह व्यक्ति, समूह, वस्तु,
परिस्थिति या फिर किसी घटना के प्रति अनुकूल या प्रतिकूल दृष्टिकोण अथवा विचार को प्रकट करता है मनोवृत्ति का प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार पर पड़ता है इसीलिए अभिवृत्ति एक मानसिक दशा है
जो सामाजिक व्यवहार की अभिव्यक्ति करने में विशेष ( महत्वपूर्ण ) भूमिका निभाती हैं मनोवृत्ति ( Attitude ) मनुष्यों के विचारों एंव फीलिंग्स को इंगित करता हैं यह बताता है कि व्यक्ति क्या महसूस करता है?, उसके पूर्व विश्वाश क्या हैं?
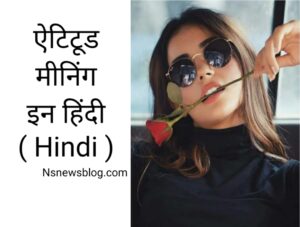
सरल भाषा ( परिभाषा ) – मनोवृत्ति ( Attitude ) का मतलब मनुष्य/व्यक्ति के उस दृष्टिकोण ( Drishtikon ) से होता हैं जिसके कारण वह व्यक्ति किन्ही परिस्थितियों, वस्तुओं, संस्थाओं, योजनाओं,
व्यक्तियों आदि के प्रति किसी विशेष प्रकार का व्यवहार करता है मनोवृत्ति के निर्माण में व्यवहार के प्रत्यक्षात्मक, प्रेरणात्मक, संवेगात्मक और क्रियात्मक पक्ष निहित रहते हैं
मनोवृत्ति सकारात्मक तथा नकारात्मक हो सकती हैं अगर किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति सकारात्मक हैं तो उसकी प्रतिक्रिया सकरात्मक/अनुकूल और अगर मनोवृत्ति नकारात्मक हैं तो प्रतिक्रिया नकारात्मक/प्रतिकूल होगी
मनोवृत्ति के घटक/ मनोवृत्ति के तत्व – Components of Attitude.
मनोवृत्ति के तीन महत्वपूर्ण घटकों/तत्वों को समझा जा सकता है जो इस प्रकार है –
- संज्ञानात्मक घटक ( Cognitive Component )
- भावनात्मक घटक ( Affective Component )
- व्यवहारात्मक घटक ( Behavioural Component )
संज्ञानात्मक घटक ( Cognitive Component ) – किसी वस्तू, व्यक्ति, वातावरण के प्रति विचारों और विश्वासों को संज्ञानात्मक घटक या तत्व कहा जाता है
भावनात्मक घटक ( Affective Component ) – किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के प्रति भाव ( घृणा, प्रेम, इर्ष्या ) से होता है भावनात्मक घटक अभिवृत्ति का सारभाग ( Core ) होता है अन्य सहायक होतें है
व्यवहारात्मक घटक ( Behavioural Component ) – किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के प्रति क्रिया करने की तत्परता को व्यवहारात्मक घटक कहा जाता हैं
Attitude Definition in Hindi – Meaning in Hindi of Attitude – Attitude in Hindi Meaning ( मनोवैज्ञानिक परिभाषाएं ).
समाज मनोवैज्ञानिकों एंव समाजशास्त्रियों ने मनोवृत्ति को परिभाषित करने के लिए मुख्य रूप से तीन दृष्टिकोणों को अपनाया है यह दृष्टिकोण ऊपर बताये मनोवृत्ति घटकों/तत्वों के ऊपर आधारित हैं
- एक विमीय दृष्टिकोण ( One-Dimensional Approach )
- द्वि-विमीय दृष्टिकोण ( Two-Dimensional Approach )
- त्रिविमीय दृष्टिकोण ( Three-Dimensional Approach )
एक विमीय दृष्टिकोण ( One-Dimensional Approach ) – इसमें मनोवृत्ति के मूल्यांकन पक्ष को ध्यान में रखकर उसे परिभाषित किया हैं इसीलिए इस दृष्टिकोण के अनुसार मनोवृत्ति एक ऐसी सीखी गई प्रवृत्ति है
जिसके कारण व्यक्ति किसी वस्तु, घटना, व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के प्रति अनुकूल/प्रतिकूल ढंग से व्यवहार करता है
आजेन और फिशवीन ( 1975 ) – इस दृष्टिकोण से मनोवृत्ति को परिभाषित किया कि किसी वस्तु के प्रति सांगत रूप से अनुकूल या प्रतिकूल ढंग से अनुक्रिया की अर्जित पूर्व प्रवृत्ति को मनोवृत्ति कहा जाता है
द्वि-विमीय दृष्टिकोण ( Two-Dimensional Approach ) – इसमें मनोवृत्ति की व्याख्या करने के लिए दो तत्वों ( संज्ञानात्मक और भावनात्मक संघटक ) का सहारा लिया गया है
इसीलिए इस दृष्टिकोण के अनुसार संज्ञानात्मक संघटक से मतलब किसी घटना का वस्तु के सम्बन्ध में व्यक्ति में जो विश्वास होता है उससे होता है और भावनात्मक संघटक का मतलब किसी वस्तु, घटना या व्यक्ति के प्रति सुखद-दुखद भाव की तीव्रता से होता है
हम उस वस्तु, व्यक्ति या घटना को पसंद करते है तथा दुखद भाव के होने पर हम उन्हें नापसंद करते है
त्रिविमीय दृष्टिकोण ( Three-Dimensional Approach ) – आधुनिक समाज मनोवैज्ञानिकों ने मनोवृत्ति की व्याख्या करने के लिए त्रिविमीय दृष्टिकोण को अपनाया
इसमें संज्ञानात्मक और भावनात्मक संघटक के साथ-साथ व्यवहारात्मक संघटक का उपयोग भी किया जाता है आधुनिक मनोवैज्ञानिकों का यह विचार अधिकतर लोगो का मान्य हैं इसीलिए इस दृष्टिकोण के अनुसार मनोवृत्ति संज्ञानात्मक संघटक,
भावनात्मक संघटक, व्यवहारात्मक संघटक तीनों का एक संगठित तंत्र है इसीलिए इसको आधुनिक समाज मनोवैज्ञानिकों एंव समाजशास्त्रियों ने मनोवृत्ति का ABC मॉडल कहा हैं जहाँ
- A – Affective Component/भावनात्मक घटक
- B – Behavioural Component/व्यवहारात्मक घटक
- C – Cognitive Component/संज्ञानात्मक घटक
फ्रीमेन – मनोवृत्ति किन्ही परिस्थितियों, व्यक्तियों या वस्तुओं के प्रति संगत ढंग से प्रतिक्रिया करने की स्वभाविक तत्परता है जिसे सीख लिया गया है तथा जो व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रतिक्रिया करने का विशिष्ट ढंग बन गया है
आलपोर्ट – मनोवृत्ति प्रत्युत्तर देने की वह मानसिक तथा स्नायुविक तत्परताओं से सम्बंधित अवस्था हैं जो अनुभव द्वारा संगठित होती है तथा जिसके व्यवहार पर निर्देशात्मक तथा गत्यात्मक प्रभाव पड़ता है
जैम्स डेवर – मनोवृत्ति मत, रूचि अथवा उद्देश्य की एक लगभग स्थायी तत्परता या प्रवृत्ति है जिसमे एक विशेष प्रकार के अनुभव की आशा और एक उचित प्रतिक्रिया की तैयारी निहित होती हैं
वुडवर्थ – मनोवृत्ति मत, रुचि या उद्देश्य की थोड़ी बहुत स्थायी प्रवृत्तियाँ है जिनमे किसी प्रकार के पूर्वज्ञान की प्रत्याशा और उचित प्रक्रिया की तत्परता निहित होती है
आईजनेक – मनोवृत्ति को किसी वस्तू/समूह के सम्बन्ध में प्रत्याक्षात्मक बाह्य उत्तेजनाओं में व्यक्ति की स्थिति और प्रत्युत्तर तत्परता के रूप में समझा जा सकता है
Drishtikon Meaning in English – Drishtikon Meaning in Hindi – Drishtikon in Hindi
दृष्टिकोण को अंग्रेजी भाषा में Attitude समझा जा सकता हैं परन्तु दृष्टिकोण का शाब्दिक अर्थ नजरिया, पहुंचना, मत होना, विचार पद्धति, अलग विचार होना होता हैं जब कोई व्यक्ति किसी विषय/बात को देखता हैं, उसको समझता हैं,
उसपर विचार करता हैं तब उस व्यक्ति का उस बात या विषय के प्रति एक दृष्टिकोण बन जाता है इसीलिए दृष्टिकोण किसी एक मुद्दें/घटना पर किसी व्यक्ति की धारणा या सोच को प्रदर्शित करता हैं
दृष्टिकोण का पर्यायवाची विचार, अंदाज़ा, राय, सोच, नजरिया, धारणा, पहलू, दृष्टि और पक्ष हो सकतें हैं

उदहारण के लिए, दो प्यार करने वालें व्यक्ति ( स्त्री और पुरुष ) भागकर शादी करना चाहतें हैं परन्तु वह दोनों मेरे ख़ास मित्र हैं इसीलिए इस स्थिति को अच्छे से समझने के बाद मैं उन दोनों मित्रों को भागकर शादी के लिए अपना दृष्टिकोण बताता हूँ
कि भागकर शादी करने से पहले हमे परिवार की सहमति के साथ यह शादी हो जाए? के ऊपर ध्यान देना चाहिए उसके बाद बात न बनने पर हमारा प्लान B ( भागकर शादी करना ) होना चाहए
मनोवृत्ति का विकास और निर्माण ( Formation of Attitude ).
मनोवृत्ति एक अर्जित प्रवृत्ति हैं समाज मनोवैज्ञानिकों ने मनोवृत्ति के विकास को प्रभावित करने वाले बहुत से कारकों से सम्बंधित कई प्रयोग किये हैं अलग अलग प्रयोगों के आधार पर इन लोगो ने निष्कर्ष के रूप में कुछ ऐसे कारकों को बताया है
जिससे मनोवृत्ति का विकास एंव उसका निर्माण प्रभावित होता है यह इस प्रकार है –
आवश्यकता पूर्ति – देखा जाता है कि जिस व्यक्ति, वस्तु, घटना से हमारे लक्ष्य की प्राप्ति होती है या आवश्यकता की पूर्ति होती है
उसके प्रति हमारी मनोवृत्ति अनुकूल होती है और जिस व्यक्ति, वस्तु, घटना से हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में बांधा उत्पन्न होती है या आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है उनके प्रति हमारी मनोवृत्ति प्रतिकूल हो जाती है
व्यक्तित्व कारक – मनोवृत्ति के निर्माण एंव विकास में व्यक्तिव शीलगुणों का भी अधिक प्रभाव पड़ता है व्यक्ति उन मनोवृत्तियों को जल्द सीख लेता हैं जो उसके व्यक्तित्व के शीलगुणों के अनुकूल होती हैं
दी गयी सूचनाएँ – मनोवृत्ति के निर्माण में व्यक्ति को दी गयी सूचनाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है आधुनिक समाज में अलग-अलग माध्यमों ( टीवी, अखबार, रेडियों, पत्रिकाएँ ) से व्यक्ति को सूचनाएँ दी जाती है जिनके अनुसार व्यक्ति अपना मनोवृत्ति विकसित करता है
मनोवृत्ति के उदाहरण के लिए, माता-पिता, भाई-बहन साथियों एंव पड़ोसियों से भी व्यक्ति को सूचना मिलती है जिसके अनुसार व्यक्ति मनोवृत्ति का विकास करता है
मेयर्स ( 1988 ) – यदि सूचना देने वाले स्त्रोत पर व्यक्ति को पूरा विश्वास होता है तब ऐसी परिस्थिति में दी गयी सूचना शत-प्रतिशत प्रभावकारी होती है एंव नयी मनोवृत्ति के विकास में सहायक होती है
सांस्कृतिक कारक – प्रत्येक संस्कृति का अपना मानदण्ड, मूल्य, परम्पराएँ, धर्म आदि होतें हैं प्रत्येक व्यक्ति का पालन-पोषण किसी न किसी संस्कृति में ही होता है
फलस्वरूप उसका समाजीकरण इन्ही सांस्कृतिक कारकों द्वारा अधिक प्रभावित होता है व्यक्ति अपनी मनोवृत्ति इन्ही सांस्कृतिक प्रारूप के अनुसार विकसित करता हैं एक समाज की संस्कृति दुसरे समाज की संस्कृति से भिन्न होती हैं
सामाजिक सीखना – सामाजिक सीखना का प्रभाव भी मनोवृत्ति के विकास में बहुत पड़ता हैं समाज मनोवैज्ञानिकों के द्वारा किये गए अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि मनोवृत्ति के विकास में सीखने के तीन तरह की प्रक्रियाओं का महत्वपूर्ण स्थान है
- क्लासिकी अनुबंधन ( Classical Conditioning )
- साधनात्मक अनुबंधन ( Instrumental Conditioning )
- प्रेक्षणात्मक अनुबंधन ( Observational Conditioning )
समूह बंधन – व्यक्ति की मनोवृत्ति के निर्माण में समूह बंधन का प्रभाव पड़ता है समूह बंधन का मतलब व्यक्ति का किसी ख़ास समूह के साथ सम्बन्ध कायम करने से होता है यह निश्चित है कि जब व्यक्ति अपना सम्बन्ध किसी ख़ास समूह से जोड़ता हैं
तब वह उस समूह के मूल्यों, मानदण्डो, विश्वासों, तौर-तरीकों को भी स्वीकार करता है ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति इन मूल्यों एंव मानदंडो के स्वरूप के अनुसार खुद में एक नयी मनोवृत्ति विकसित करता है
मनोवृत्ति की प्रकृति/अभिवृत्ति की प्रकृति – Nature of Attitude.
मनोवृत्ति की प्रकृति को तीन प्रकारों के माध्यम से समझा जा सकता हैं जो इस प्रकार हैं –
- धनात्मक ( Positive )
- ऋणात्मक ( Negative )
- शून्य ( Zero )
धनात्मक – इसमें किसी भी सम्बंधित व्यक्ति, घटना, समूह के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण ही धनात्मक प्रवृत्ति की अभिवृत्ति हैं
ऋणात्मक – इसमें व्यक्ति, समूह या घटना के प्रति ऋणात्मक दृष्टिकोण पाया जाता है और यही ऋणात्मक दृष्टिकोण ऋणात्मक प्रवृत्ति की अभिवृत्ति हैं
शून्य – यह अभिवृत्ति न तो सकारात्मक होती है और न ही नकारात्मक होती हैं किसी व्यक्ति, समूह या घटना के प्रति किसी भी प्रकार की कोई मनोवृत्ति न होना शून्य अभिवृत्ति कहलाता हैं
अभिवृत्ति के प्रकार/मनोवृत्ति के प्रकार – Types of Attitude in Hindi.
मनोवृत्ति के प्रकारों को समझने के लिए हम नीचे बताये कुछ प्रकारों को पढ़कर समझ सकतें हैं जो इस प्रकार है –
- मानसिक अभिवृत्ति
- विशिष्ट अभिवृत्ति
- सकरात्मक अभिवृत्ति
- सामान्य अभिवृत्ति
- नकारात्मक अभिवृत्ति
मानसिक अभिवृत्ति – मानसिक रूप से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के सम्बन्ध में अलग-अलग अभिवृत्ति होती है इन्हें अनेक क्षेत्र के नाम से ही पुकारते है उदहारण के लिए, सामाजिक अभिवृत्ति, सौन्दर्यनुभूति अभिवृत्ति, धार्मिक अभिवृत्ति. इसी प्रकार प्रत्येक क्षेत्र से सम्बंधित अभिवृत्ति हो सकती हैं
विशिष्ट अभिवृत्ति – जो अभिवृत्ति किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, विचार तथा संस्था विशेष के प्रति व्यक्त की जाती हैं विशिष्ट अभिवृत्ति कहलाती हैं उदहारण के लिए, छात्र अपने शिक्षक के प्रति जो सम्मान और श्रद्धा प्रकट करता है वह उसकी विशिष्ट अभिवृत्ति होती हैं
सकरात्मक अभिवृत्ति – जब किसी व्यक्ति, विचार, घटना या संस्था आदि की उपस्थिति हमे सुखद लगती हैं और उसके प्रति हमारी अनुकूल प्रतिक्रिया होती है तथा जब हम उसके पक्ष में बोलते है तब हमारी सकारात्मक अभिवृत्ति होती है
मतलब जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति, संस्था, विचार, धर्म प्रक्रिया के प्रति विश्वास रखतें है,
उसे पसंद करते है, स्वीकार करते है, उसके प्रति आकर्षित होतें है तथा उसके अनुकूल खुद को समायोजित ( Adjust ) करने की चेष्टा करते है वह हमारी सकारात्मक अभिवृत्ति कहलाती है
सामान्य अभिवृत्ति – सामान्य अभिवृत्ति वह होती है जो अभिवृत्ति व्यक्ति, वस्तु, घटना, विचार आदि के बारे में सामान्य या सामूहिक रूप से व्यक्त की जाती है
उदहारण के लिए, घड़ियों के विषय में अभिवृत्ति, राजनैतिक दलों के बारे में दृष्टिकोण या रेल दुर्घटनाओं के प्रति अभिवृत्ति आदि
नकारात्मक अभिवृत्ति – जब हमारा दृष्टिकोण किसी वस्तु, घटना या विचार के प्रति सुखद नहीं होता है या हम उसे पसंद नहीं करतें हैं और उसके प्रति उत्तेजनात्मक प्रतिक्रिया करते है तब वह नकारात्मक अभिवृत्ति कहलाती है
इस प्रकार जब हम किसी राजनैतिक पार्टी, प्रक्रिया, जाति, स्थान या व्यक्ति से घृणा करते हैं, उनके निराश होतें हैं, उनमे अविश्वाश रखते है तथा अपने को दूर रखने का प्रयास करते हैं वह नकारात्मक अभिवृत्ति कहलाती हैं
मनोवृत्ति की विशेषताएँ – Characteristics of Attitude.
अभिवृत्ति की निमंलिखित विशेषताएँ होती है जो इस प्रकार हैं –
- यह व्यवहार को प्रभावित करती हैं मतलब एक व्यक्ति की अभिवृत्तियों का प्रभाव दुसरे व्यक्ति की अभिवृत्ति पर पड़ता है
- अभिवृत्तियों का विकास सामाजिक संबंधों के कारण होता है और यह व्यक्तिगत एंव सामाजिक दोनों प्रकार की होती हैं
- अभिवृत्ति भावनाओं की गहराई का स्वरूप है क्योकि मनोवृत्ति का सम्बन्ध व्यक्ति की भावनाओं की गहराई से होता है और यह किसी व्यक्ति, घटना, विचार या वस्तु के प्रति अनुकूल अथवा प्रतिकूल भावना का प्रदर्शन करती है
- मनोवृत्ति व्यक्ति के व्यवहार का प्रतिबिम्ब होती है इसीलिए हम किसी मनुष्य के व्यवहार को देखकर उसकी अभिवृत्ति के बारे में पता कर सकतें है
- अभिवृत्ति का स्वरूप स्थायी होता है तथा एकरूप होता है परन्तु अभिवृत्ति को अधिक समय में बदला जा सकता है इसीलिए यह अपना रूप बदल भी देती है
- अभिवृत्ति के सामाजिक तथा मानसिक दोनो पक्ष होतें हैं और अभिवृत्ति का सम्बन्ध व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों बुद्धि, मानसिक, प्रतिभा एंव विचारों से होता है
- अभिवृत्ति जन्मजात नहीं होती है बल्कि यह अर्जित की जाती हैं और यह अनुभवों के आधार पर अर्जित होती हैं तथा वस्तुओं, मूल्यों एंव व्यक्तियों के संबंध में सीखी जाती है
- यह सदैव परिवर्तनशील होती हैं और यह सदैव संवेगों तथा भावों से प्रभावित होती हैं अभिवृत्ति का सम्बन्ध समस्याओं तथा आवश्यकताओं से होता है
एटीट्यूड का मतलब घमंड होता है क्या? Attitude Ka Matlab – Attitude Hindi Meaning – Attitude Meaning Hindi.
नहीं, एटीट्यूड का मतलब घमंड नहीं होता है क्योकि जब हमारे पास पैसा, गाडी, बंगला या एक अच्छी लाइफस्टाइल होती हैं तब ऐसी स्थिति में कुछ मनुष्य को अपनी अच्छी लाइफस्टाइल पर थोडा या ज्यादा घमंड होता है
परन्तु यह स्थिति उस मनुष्य के एटीट्यूड को नहीं दिखाती है बल्कि एटीट्यूड एक तरह का व्यवहार होता है जो हम किसी दुसरे मनुष्य से मिलने पर करतें हैं हमारा एटीट्यूड इस बात पर निर्भर करता है कि हम जिस मनुष्य से मिल रहें है

उस मनुष्य के लिए हमारा नजरिया/दृष्टिकोण/रवैया कैसा हैं? हमारा एटीट्यूड हमारी सोच को दिखाता हैं
उदहारण के लिए, अगर आप किसी लड़की के सामने उसके आत्मनिर्भर होने पर गलत व्यवहार करतें हैं तब ऐसी स्थिति में आपका यह व्यवहार उस लड़की या आस-पास के अन्य मनुष्यों को लड़की के आत्मनिर्भर होने के प्रति आपकी ख़राब सोच को दिखाता है
अभिवृत्ति, रूचि, मूल्य, अभिप्रेरणा, अभिक्षमता में अंतर लिखिए?
अभिवृत्ति एंव रूचि के लिए,
अभिवृत्ति एंव रूचि दोनों एक ही व्यक्तित्व के पहलू हैं, परन्तु मापने की दृष्टि से दोनों में बहुत अंतर हैं क्योकि अभिवृत्ति व्यक्ति की दोनों प्रतिक्रियाओं सुख-दुःख, सकारात्मक-नकारात्मक, अनुकूल-प्रतिकूल, स्वीकृति-अस्वीकृति को दर्शाती हैं
जबकि रूचि केवल एक ही पहलू की ओर संकेत करती है रूचि में व्यक्ति केवल अपनी पसंद को प्राथमिकता देता है इस प्रकार अभिवृत्ति का क्षेत्र रूचि से अधिक व्यापक है
अभिवृत्ति एंव मूल्य के लिए,
अभिवृत्ति एंव मूल्य दोनों व्यक्ति के मानसिक तत्व है परन्तु दोनों में कुछ भिन्नता पायी जाती है जहाँ एक तरफ अभिवृत्ति आत्मगत होती है वही दुसरी तरफ मूल्य वस्तुगत होते है दुसरे शब्दों में मूल्य का महत्त्व अधिक होता है
इस प्रकार अभिवृत्ति किसी वस्तु की ओर इंगित करने वाली प्रवृत्ति का नाम है लेकिन जब यह अभिवृत्ति लक्ष्य बन जाती है तब वह मूल्य का रूप धारण कर लेती है मतलब मूल्य का स्वरूप समाज के हित के लिए होता है
अभिवृत्तियाँ व्यक्तिगत भी हो सकती है लेकिन मूल्य की व्यापकता अभिवृत्तियाँ से अधिक होती हैं इसीलिए अभिवृत्तियाँ मूल्यों का आधार होती है मूल्य का प्रत्यक्ष रूप से माप संभव नहीं है जबकि अभिवृत्तियों का वैज्ञानिक माप संभव होता है
अभिवृत्ति एंव अभिप्रेरणा के लिए.
अभिवृत्ति एंव अभिप्रेरणा दोनों ही व्यवहार की क्रिया है इनका सम्बन्ध किसी न किसी लक्ष्य से होता है दोनों में संवेगात्मक एंव प्रत्यक्षात्मक गुण निहित होते है परन्तु दोनों में फिर भी कुछ भिन्नताएँ पायी जाती है
अभिवृत्ति, अभिप्रेरणा से अधिक स्थायी होती है अभिवृत्ति व्यक्ति में सदैव विद्धमान रहती है लेकिन अभिप्रेरणा केवल निश्चित समय पर ही उत्पन्न होती है उदहारण के लिए, भूख की अभिप्रेरणा भोजन मिलने जाने पर समाप्त हो जाती है और,
कुछ समय बाद फिर जाग्रत हो जाती है, लेकिन भोजन सम्बन्धी व्यजनों के प्रति पसंद और नापसंद की अभिवृत्ति सदैव बनी रहती हैं इस प्रकार अभिवृत्ति का क्षेत्र अभिप्रेरणा से व्यापक है एक अभिवृत्ति में अनेक अभिप्रेरणाएँ होती है
अभिवृत्ति एंव अभिक्षमता के लिए,
अभिवृत्ति उस व्यक्तित्व की ओर इंगित करती है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, संस्था अथवा प्रत्यय के प्रति अपने विचार व्यक्त करते है जबकि अभिक्षमता इन विशेषताओं का सम्मिश्रण है जो विशिष्ट कैशल के सीखने में व्यक्ति की योग्यताओं की ओर संकेत करती है
अभिवृत्ति सदैव अर्जित होती है जबकि अभिक्षमता अर्जित एंव जन्मजात दोनों ही प्रकार की होती हैं
इगो और एटीट्यूड में क्या अंतर है?
इगो और एटीट्यूड दोनों किसी मनुष्य के सामने हमारी पहचान बन सकतें हैं क्योकि इगो और एटीट्यूड दोनों मनुष्य के द्वारा किया जाने वाला व्यवहार है परन्तु अगर आपका इगो कम हैं तब यह एटीट्यूड हो सकता है
परन्तु किसी मनुष्य के लिए आपके अंदर अत्यधिक इगो हैं तब यह आपके लिए अहंकार का रूप लेता हैं उसके बाद आप अपने आगें उस मनुष्य को बहुत छोटा, कमजोर समझने लग जातें हैं
उदहारण के लिए, अगर आप किसी मनुष्य की मदद अपने इगो के कारण नहीं करतें है तब ऐसी स्थिति में आप उसके सामने अपनी मुसीबत में मदद न करने की छवि का निर्माण कर रहें हैं
उसके बाद उस व्यक्ति का आपके प्रति एटीट्यूड बदल जाता हैं और वह आपसे बात करने से बचता है क्योकि आप उसके दिल को पसंद नहीं आयें हैं उसकी नजरों में आपकी यह पहचान बन गई हैं
लेकिन अगर आप अपने सकारात्मक एटीट्यूड ( व्यवहार ) के साथ मुसीबत में उसकी मदद कर देते है तब आप दोनों कुछ मिनटों में एक अच्छे दोस्त बन जातें हैं
मनोवृत्ति का मापन – अभिवृत्ति का मापन – Measurement of Attitude ( Manovriti Meaning in Hindi ).
अभिवृत्ति का मापन बहुत कठिन हो जाता हैं क्योकि अभिवृत्ति की प्रकृति आंतरिक होती हैं और व्यक्ति के मनोभाव से सम्बंधित होती है फिर भी समय-समय पर आवश्यकताओं के अनुसार अभिवृत्तियों के मापन के विभिन्न प्रयास किये गए हैं
अभिवृत्ति मापन के इतिहास से यह स्पष्ट होता है कि अभिवृत्तियों के मापन के प्रयास अपेक्षाकृत नये है और लगभग सात दशक पूर्व ही अभिवृत्ति मापन के लिए प्रविधियां विकसित की गई थी
इसमें पहले साक्षात्कार एंव अवलोकन की सहायता से ही अभिवृत्तियों का मापन किया जाता था वर्ष 1927 में थर्सटन ने तुलनात्मक नियम का प्रतिपादन किया अभिवृत्ति मापन की विधियों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है
- व्यवहारिक प्रविधियां
- मनोवैज्ञानिक प्रविधियां
व्यवहारिक प्रविधियां – व्यवहारिक विधियों में व्यक्ति से सीधे-सीधे प्रश्न पूछ कर या उसके व्यवहार का प्रत्यक्ष अवलोकन करके उसकी अभिवृत्तियों को जाना जाता हैं
- प्रत्यक्ष प्रश्न विधि ( Direct Questioning )
- व्यवहार के प्रत्यक्ष निरिक्षण विधि ( Direct Observation )
प्रत्यक्ष प्रश्न विधि ( Direct Questioning )
प्रत्यक्ष प्रश्न विधि में किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के प्रति अभिवृत्ति को ज्ञात करने के लिए सीधे-सीधे प्रश्न पूछे जातें है व्यक्ति द्वारा दिए गए प्रश्नों के उत्तरों के आधार पर अभिवृत्ति से सम्बंधित जानकारी हमे प्राप्त होती हैं
इस मेथड में अभिवृत्ति का मापन तीन वर्गों में किया जा सकता है
- ऐसे व्यक्ति जिनकी अनुकूल अभिवृत्ति हैं
- ऐसे व्यक्ति जिनकी अभिवृत्ति प्रतिकूल हैं
- ऐसे व्यक्ति जो यह कहतें है कि वे अभिवृत्ति के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट मत नहीं बना पा रहें हैं
व्यवहार के प्रत्यक्ष निरीक्षण विधि ( Direct Observation )
अभिवृत्ति ज्ञात करने की प्रत्यक्ष निरीक्षण विधि में व्यक्तियों के व्यवहार का निरीक्षण करके उनकी अभिवृत्ति का पता लगाया जा सकता है इस मेथड में व्यक्ति द्वारा अपने दिन-प्रतिदिन की दिनचर्या के दौरान किये जाने वाले व्यवहार के द्वारा किसी वस्तु,
व्यक्ति और संस्था के प्रति उसकी अभिवृत्ति को ज्ञात किया जा सकता है इस विधि के द्वारा भी व्यक्तियों को उनकी अभिवृत्ति के आधार पर तीन वर्गों में बाटा गया है
- अनुकूल अभिवृत्ति
- प्रतिकूल अभिवृत्ति
- अनिश्चित अभिवृत्ति
यह विधि प्रत्यक्ष प्रश्न विधि की तुलना में अधिक उपयुक्त विधि है क्योकि इसमें व्यक्ति को यह आभास ( पता ) ही नहीं हो पाता है कि उसका निरीक्षण हो रहा है
मनोवैज्ञानिक प्रविधियां – जब प्रचलित विधियों में कुछ कमी रह जाती है तब नयी विधियों का जन्म होता है इसीतरह अभिवृत्ति मापन की व्यवहारिक विधियों की कमी के कारण मनोवैज्ञानिक विधियों ने जन्म लिया था
इसीलिए अभिवृत्ति मापन के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जा रहा है
- युग्म तुलनात्मक विधि ( द्वारा – थर्सटन 1927 )
- मास्टर टाइप मापनी ( द्वारा – रैमर्स )
- सम-दृष्टि अंतर विधि ( द्वारा – थर्सटन और चेब )
- स्केलोग्राम विधि ( द्वारा – गट्मैन 1945 )
- योग निर्धारण विधि ( द्वारा – लिकर्ट 1932 )
- सिमेंटिक डिफरेंशियल विधि ( द्वारा – ओसगुड 1952 )
- क्रमबद्ध अंतर विधि ( द्वारा – सफीर 1937 )
- भेद बोधक मापनी विधि ( द्वारा – एडवर्स और किलपैट्रिक 1948 )
युग्म तुलनात्मक विधि ( द्वारा – थर्सटन 1927 )
इस विधि का विकास वर्ष 1927 में थर्सटन के द्वारा किया गया था थर्सटन ने युग्म रूप से कुछ कथनों की सूची तैयार किया और छात्रों से प्रत्येक जोड़े में दिए गए कथनों में से उसकी सहमति किसके साथ हैं या उसकी असहमति किसके साथ है,
यह जानने का प्रयास किया गया इस विधि में प्रत्येक कथन को किसी अन्य कथनों के साथ उसको जोड़कर युग्म तैयार किया गया साथ ही सभी जोड़ो के सम्बन्ध में उनकी सहमति या असहमति पुछी जाती हैं
इसीलिए इस विधि में व्यक्ति को एक ही समय में दो कथनों के जोड़े के रूप में विभिन्न मिश्रणों के साथ तुलना करनी होती है तथा व्यक्ति को दोनों कथनों के प्रति अपना निर्णय देना होता है इसीलिए अभिवृत्ति मापन के लिए यह सबसे अच्छी विधि होती हैं
Thurstone Scales – इसको Equal Appearing Interval Scale भी कहा जाता है क्योकि इसका उपयोग किसी दिए गए अवधारणा या निर्माण के प्रति दृष्टिकोण को मापने के लिए किया जाता है
इसका उपयोग किसी विषय के प्रति प्रतिवादी के व्यवहार, दृष्टिकोण या भावना को ट्रैक करने के लिए किया जाता है इस पैमाने में किसी विशेष मुद्दे या विषय के बारे में कथन होतें है जहाँ प्रत्येक कथन का एक संख्यात्मक मान होता है
जो विषय के प्रति उत्तरदाताओं के रवैये को अनुकूल या प्रतिकूल के रूप में इंगित करता है
मास्टर टाइप मापनी ( द्वारा – रैमर्स )
रैमर्स ने अनुकूलता के घटते हुए क्रम में अभिवृत्ति मापन की मास्टर टाइप मापनी की रचना की अभिवृत्ति मापनियों की विश्वसनीयता एंव वैधता अधिकांशत: अभिवृत्ति मापनियों की विश्वसनीयता का सम रूपान्तर और,
सम-विषय प्राप्तांक विधि द्वारा ज्ञात किया जा सकता है विभिन्न अभिवृत्ति मापनियों की विश्वसनीयता में बहुत अंतर दृष्टिगोचर होता है कुछ की मध्यांक विश्वसनीयता सत्तर ( 70 ), कुछ की साठ ( 60 ) और अन्य की पचास ( 50 ) से भी कम ज्ञात की गई
थर्सटन और लिकर्ट विधियों की विश्वसनीयता को नब्बे ( 90 ) पाया गया सांख्यिकीय विधियों से अभिवृत्ति मापनी की वैधता जानने के लिए इनके दो पदों को देखकर इनकी वैधता को ज्ञात किया जा सकता है
सम-दृष्टि अंतर विधि ( द्वारा – थर्सटन और चेब )
मनोविज्ञान में इस विधि का प्रतिपादक थर्सटन ने चेब के साथ मिलकर किया था इस विधि में कुछ कथन होतें है किन्तु उनकी संख्या अधिक होती है कथन जोड़ों में न होकर स्वतंत्र रूप से होता है
प्रत्येक प्रश्न पर व्यक्ति की अनुकूल, प्रतिकूल और तटस्थ स्थिति की सहमति पूछी जाती है यह सहमति/असहमति 11 ( ग्यारह ) बिन्दुओं वाले निर्धारण मापनी पर पूछी जाती है
स्केलोग्राम विधि ( द्वारा – गट्मैन 1945 )
गट्मैन ने एक नई विधि का प्रतिपादन वर्ष 1945 में किया था जिसका नाम स्केलोग्राम विधि रखा गया इस विधि में भी कथनों को जोड़ों में दिया जाता है सहमति की मात्रा जितनी अधिक होगी अभिवृत्ति अंक उतने ही अधिक होंगे
इस विधि में व्यक्ति के कथन के बारे में केवल सहमति या असहमति ही पूछी जाती है सहमति की स्थिति में एक ( 1 ) अंक तथा असहमति की स्थिति में ( 0 ) अंक प्रदान करके सबका योग करके कुल अभिवृत्ति अंक प्राप्त कर लेते हैं
Guttman Scaling – गट्मैन स्केलिंग, जिसको स्केलोग्राम विश्लेषण भी कहा जाता है यह इस विचार पर आधारित है कि वस्तुओं को एक निरंतरता के साथ इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि एक व्यक्ति जो किसी वस्तु से सहमत हैं
वह अन्य सभी वस्तुओं से भी सहमत होगा उदहारण के लिए,
- पहला उदहारण – टीवी पर अश्लील प्रोग्राम समाज के लिए हानिकारक है
- दुसरा उदहारण – बच्चो को अश्लील टीवी शो देखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए
- तीसरा उदहारण – टेलीविजन स्टेशन प्रबंधकों को अपने स्टेशनों पर अश्लील कार्यक्रम की अनुमति नहीं देनी चाहिए
- चौथा उदहारण – सरकार को टीवी से अश्लील प्रोग्राम पर प्रतिबंध लगाना चाहिए
निष्कर्ष – अगर कोई व्यक्ति पहला उदहारण से सहमत हैं तब वह अन्य दुसरा, तीसरा, चौथा उदहारण से भी सहमत होगा
योग निर्धारण विधि ( द्वारा – लिकर्ट 1932 )
इस विधि को लिकर्ट के द्वारा वर्ष 1932 में विकसित किया गया था क्योकि उन्होंने यह देखा कि थर्सटन और चेब के द्वारा बनाई गई समान उपस्थिति अंतराल विधि या सम–दृष्टि अंतर विधि में समय कम या बहुत अधिक लगता है
इसमें पूर्ण प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होती हैं यह काफी कठिन कार्य हैं तो लिकर्ट ने एक सरल ( आसान ) विधि का निर्माण किया जिसमे भी निर्धारण मान का प्रयोग किया जाता है
परन्तु इसमें निर्धारण मान ग्यारह ( 11 ) बिन्दुओं की जगह सिर्फ पाँच ( 5 ) बिन्दुओं को रखा जाता है
- पूर्ण सहमति
- सहमति
- अनिश्चित
- असहमति
- पूर्ण अहसमति
Likert Scale – इसको Summated Rating Scale भी कहा जाता है किसी विषय के सम्बन्ध में कई कथन विकसित किये जाते है और उत्तरदाता दृढता से सहमत हो सकतें है, तटस्थ हो सकतें है, असहमत हो सकतें है या बयान से असहमत हो सकतें है
सिमेंटिक डिफरेंशियल विधि ( द्वारा – ओसगुड 1952 )
इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1952 में ओसगुड के द्वारा किया गया था यह स्कूल स्वीकार करके चलता है कि एक ही मनोवैज्ञानिक पदार्थ के प्रति विभिन्न व्यक्तियों की विभिन्न धारणा होती है धारणा में विभिन्नता व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण होती है
इस मान्यता को लेकर ओसगुड ने अनेक कथन बनाये जिनका वर्णन तथा निर्णय को एक निर्धारित मान पर प्रदर्शित किया गया था इस निर्धारण मान के सात स्थान होतें है तथा प्रत्येक व्यक्तिगत दो विपरीत शब्दों में व्यक्त किया होता है
Semantic Differetial Scales – यह एक स्केलिंग प्रक्रिया है जैसा कि मूल रूप से ओसगुड, सूसी और टेननबाम ( 1957 ) में कल्पना की थी इस तकनीक का उपयोग किसी व्यक्ति के लिए एक आइटम के अर्थ को मापने के लिए किया जाता है
इस तकनीक का उपयोग करने के लिए, द्वि-ध्रुवी दृष्टिकोण द्वारा सात ( 7 ) बिंदु पैमाने की एक श्रृंखला तैयार की जाती है जिसके शीर्ष पर एक नाम या एक अवधारणा रखी होती है
क्रमबद्ध अंतर विधि ( द्वारा – सफीर 1937 )
इस विधि पर सबसे पहला कार्य थर्सटन ने किया था परन्तु इसके सम्बन्ध में व्यापक प्रयोग तथा प्रचार सफीर ने किया था इसीलिए इसको सफीर क्रमबद्ध अंतर विधि के नाम से जाना जाता है जिसका निर्माण वर्ष 1937 में किया गया था
इस विधि में कथन बहुत अधिक मात्रा में होतें है तथा कथनों को क्रम अंतर में मापा जाता है प्रत्येक कथन का आवृत्ति विवरण यह बताता है कि कथनों की कितनी पुनरावृत्ति हुई हैं
भेद बोधक मापनी विधि ( द्वारा – एडवर्स और किलपैट्रिक 1948 )
इस विधि को वर्ष 1948 में एडवर्स और किलपैट्रिक के द्वारा प्रतिपादन किया था यह विधि भौतिक विधि नहीं हैं इसीलिए इसमें उपलब्ध समान विधियों को मिलाकर एक नया रूप प्रस्तुत किया गया है
इस विधि को प्रमुख रूप से समान उपस्थिति विधि तथा भेद बोधक मापनी विधि कहतें हैं
धनात्मक अभिवृत्ति क्या है? धनात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने के उपाय लिखिए?
धनात्मक अभिवृत्ति का महत्व बहुत ख़ास होता है लगभग हर व्यक्ति के मन में यह सवाल रहता है कि एक अच्छा एटीट्यूड क्या होता है?
बचपन से हमारे माता-पिता हमें शिष्टाचार सीखाना शुरू करतें है जिससे उनके बच्चें ( हम ) एक अच्छे इंसान बनें हमें खुद से बड़ों का सम्मान करना, छोटों के साथ प्यार ( प्रेम ) से बात करना आदि सीखाया जाता है
लेकिन मनुष्य उम्र के किसी भी नंबर पर होकर लाइफ में अपने एटीट्यूड को बेहतर बना सकतें हैं मनोविज्ञानिकों के मुताबिक़ एटीट्यूड बहुत छोटी चीज हैं लेकिन इसका महत्व बहुत अधिक होता है
अगर कोई व्यक्ति हमसे यह कहता है कि आपमें बहुत एटीट्यूड हैं? एक पॉजिटिव एटीट्यूड या धनात्मक अभिवृत्ति का मतलब सिर्फ अपने चेहरे पर मुस्कान रखना नहीं होता है यह आपके बेहतर रवैया को प्रदर्शित करता है
जब सभी चीजे आपके कण्ट्रोल से बाहर होती है ऐसी स्थिति में भी जब आप सिर्फ पॉजिटिव सोचतें हैं और अच्छी बातों को देखने की कोशिश करतें हैं तब यह कहा जा सकता है कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड या धनात्मक अभिवृत्ति रखतें हैं
एटीट्यूड क्या दिखाता हैं –
- आप खुद के बारे में क्या सोचतें हैं?
- आप दूसरों को किस नजरिये से देखतें है?
- दूसरों के बारे में आपका क्या रवैया हैं?
- जब कोई आपसे बात करता है तब आपके दिमाग में सबसे पहला विचार क्या आता है?
अगर आप किसी व्यक्ति से बातचीत करने के दौरान उसके लिए अच्छा सोचतें है, ख़राब से ख़राब परिस्थिति में भी आप खुद को पॉजिटिव बनायें रखतें हैं तब यह आपका पॉजिटिव एटीट्यूड कहलाता है
लेकिन जब आप अपने जीवन के हर एक पड़ाव में सिर्फ मुश्किलों को देखतें हैं, आपके सामने हमेशा चीजें बेकार दिखाई देती हैं और आप चीजों में सिर्फ बुरी चीजें देखतें हैं इसका मतलब यह होता है कि आपका एटीट्यूड बहुत अधिक नेगेटिव हैं

उदहारण के लिए, अगर आप एक इंटरव्यू के लिए खुद को तैयार कर रहें है और आप इंटरव्यू देने की जगह पहुंचकर वहाँ बैठे लोगो को देखकर यह सोचने लगते है कि यह लोग बहुत अच्छे दिखाई दे रहें है? इनको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं है
मैं शायद अच्छा नहीं दिखाई दे रहा हूँ यह स्थिति आपके नकारात्मक एटीट्यूड या ऋणात्मक अभिवृत्ति को दिखाता है यहाँ आप इंटरव्यू देने से पहले अपने नकारात्मक एटीट्यूड के कारण हार मान चुके हैं
ऐसी स्थिति में आपके असफल होने की संभावना अधिक है परन्तु अगर इस स्थिति में आप खुद को पॉजिटिव रखतें हैं तब आप अपने सफल होने की संभावना को बढ़ा देतें हैं क्योकि यहाँ आपका कॉन्फिडेंस अधिक हो जाता है
धनात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने के उपाय लिखिए?
- किसी भी कार्य को करने से पहले यह नहीं सोचना चाहिए कि मुझसे नहीं हो पायेगा
- लाइफ में समस्या पर नहीं बल्कि समस्या के उपाय पर अधिक फोकस रखना चाहिए
- हर मनुष्य के लिए मन में अच्छा सोचना शुरू करें
- जीवन में जरूरतमंद मनुष्यों की मदद करना अच्छा होता है क्योकि यह कार्य आपको पॉजिटिव रहने में मदद करता है
- हर खराब परिस्थिति में, आस-पास अधिक से अधिक नकारात्मक व्यक्ति होने पर, सभी लोग आपके खिलाफ हो जाए तब भी आपको अपनी पॉजिटिव अभिवृत्ति को बनाये रखना होगा
- लाइफ में मेहनत करके कामयाबी या सफलता मिलने पर उसका जश्न बनाना जरुरी हैं यहाँ आप रोजाना के कार्यों में हर छोटी-बड़ी उस चीज को ढूढ़ सकतें है जिससे आपको ख़ुशी मिली हो
- हमेशा उन लोगो का साथ ढूढना हैं जो अच्छी और धनात्मक सोच रखतें है और आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करतें है
- अपनी क्षमता का विकास करने के लिए कार्य करें क्योकि ऐसा करने से हमारा आत्मविश्वास प्रबल होता है
- खुद के रवैये को सकारात्मक या पॉजिटिव बनाने के लिए आपको हमेशा अच्छा बोलना चाहिए, लोगो के साथ बहस करने से हमेशा बचना चाहिए
- हमारे पास जितना है, जो कुछ भी हैं उसके लिए हमेशा भगवान् के आभारी रहना चाहिए
- जब आपके दिमाग में कोई नकारात्मक ख्याल आता है तब आप उसको तुरंत किसी सकारात्मक ख्याल में बदलने का प्रयास करें क्योकि नकारात्मक ख्याल, धनात्मक अभिवृत्ति को कमजोर करतें है
- किसी मनुष्य से बात करने के दौरान पहले उसको ठीक से सुने, सोचें उसके बाद प्रतिक्रिया देनी चाहिए
- हमेशा खुश रखे का प्रयास करना चाहिए, अगर कोई कार्य आपके हिसाब से नहीं हो रहा है तब भी आपको गुस्सा करने से बचना चाहिए हर समय खुश रहने के लिए आप ख़राब परिस्थिति में जो अच्छा हुआ हैं उसके बारे में अधिक सोचें
Attitude Dialogue in Hindi – Attitude Shayari in Hindi – Status about Attitude in Hindi – Attitude Shayari.
अक्सर कुछ व्यक्ति एटीट्यूड इन हिंदी शायरी ( Attitude Status in Hindi ) सर्च करके सोशल मीडिया या फिर रियल लाइफ में उपयोग करके के लिए एटीट्यूड स्टेटस सर्च करने लग जाते हैं क्योकि हमने एटीट्यूड विषय पर गहरा अध्ययन किया है
यही कारण है कि इस विशेष लेख में आपको कुछ ऐसे यूनिक एटीट्यूड स्टेटस दिए जाएंगे जिनका उपयोग आप सोशल मीडिया पर बिना किसी झिझक के साथ कर सकतें है
मुझे लोग नजरअंदाज नहीं करतें है अरे,
नजरों से देखने की हिम्मत नहीं होती हैं…
एटीट्यूड बहुत छोटी चीज हैं लेकिन मुझें यूनिक बनाती है,

हाँ, अलग हूँ मैं तुमसे क्योकि मुझें जीहुजूरी करनी नहीं आती हैं…
शांत रहता हूँ सोचकर कभी हद ( लिमिट ) पर मत करना,
अगर अशांत हो गया तो तुझें हमेशा के शांत करदुंगा
हाँ, बदला लेना मेरी आदत ( Habbit ) नहीं हैं परन्तु अगर,
मुझे परेशान करने की हिम्मत रखोगें तब सीधा हॉस्पिटल जाओगें…
मुझमें Ego बिल्कुल नहीं है लेकिन इज्जत मिले यह शौक हैं इसीलिए,

जब इज्जत मिलने में कंजूसी होगी तब मैं सबको नजरअंदाज कर देता हूँ…
खुद जलने का शौक नहीं है मुझें लेकिन लोग मुझसे जलते है,
आग नहीं हूँ मैं बस काम ऐसे है जो बहुत लोगो को परेशान करते है…
अखबार बदलता है, कैलेंडर बदलना है लेकिन मैं नहीं,
गद्दार झुकता है, धोखेबाज छुपता है लेकिन मैं नहीं,

महोदय आपने बहुत गलत व्यक्ति के साथ डील किया है,
मैं झुकता नहीं हूँ, छुपता नहीं हूँ, रोकता नहीं हूँ, मैं फाइटर हूँ,
लड़ता हूँ मगर डरता नहीं हूँ…
मेरा भूलने का एक नियम बहुत लोकप्रिय हैं मेरी जान,
अगर कोई अपनी औकात भूलता हैं तब मैं उसको भूल जाता हूँ…
अधिकतर लोग सोचते हैं कि मुझे कोई मिली नहीं इसीलिए अकेला हूँ लेकिन,

लोग यह नहीं जानते है कि मैं लड़कियों को नजरअंदाज करता हूँ क्योकि मैं दिलजस्प नहीं हूँ…
अमीर हूँ मैं लेकिन चप्पल पहनता हूँ,
पैसा बहुत है लेकिन बचत करता हूँ,
बड़ी गाडी है मेरे पास लेकिन कभी-कभी पैदल चलता हूँ,
एटीट्यूड बहुत अच्छा है मेरा लेकिन कुछ लोगो के सामने Bad बॉय बनता हूँ
यह चप्पल दिखाई देती हैं उसको लगता है मैं गरीब हूँ,
पगली यह नहीं जानती है कि अमीर भी चप्पल पहना करते हैं…
वह व्यक्ति अच्छा है जिसके जेब में पैसा हैं,
वह व्यक्ति स्मार्ट है जिसके दिमाग में ज्ञान है,
वह व्यक्ति दयालु है जिसके दिल में प्यार हैं,
वह व्यक्ति जिम्मेदार हैं जो जिम्मेदारी निभाता हैं,
उस व्यक्ति का एटीट्यूड अच्छा है जो पॉजिटिव, कॉन्फिडेंसम व्यक्तित्व का धनी हैं…
अभिवृत्ति के गुण और दोष लिखिए? अभिवृत्ति के गुण एवं दोष बताइए? अभिवृत्ति के दोष, अभिवृत्ति के गुण बताइए?
- हमारा पॉजिटिव मनोवृत्ति या एटीट्यूड किसी ही नकारात्मक चीज को ख़तम करता है इसीलिए नकारात्मक पारिस्थितियों में भी हमारा पॉजिटिव दृष्टिकोण को अपनाना बहुत जरुरी होता है
- अगर आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखतें हैं तब आपके लिए हर कार्य में सफलता पाना आसान होता है लेकिन नकारात्मक एटीट्यूड रखने पर किये गए हर कार्य में असफलता मिलने के चांस अधिक होतें हैं
- हमारा एटीट्यूडअच्छा होने पर अधिक से अधिक लोग हमे पसंद करतें हैं और हमारे साथ अधिक से अधिक समय बिताना पसंद करतें है लेकिन ख़राब एटीट्यूड के कारण लोगो हमे नापसंद करतें हैं और हमसे दूर भागते है
- पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा हमें आज में अच्छे और ख़ुशी के साथ जीने में मदद करती है लेकिन ऋणात्मक एटीट्यूड हमारे अतीत के माध्यम से हमारे आज को ख़राब करता है
- अच्छा एटीट्यूड रखने से हम खुद के बारे में हमेशा अच्छा महसूस करतें हैं परन्तु ख़राब एटीट्यूड के कारण हम खुद को कमजोर, बेकार, बेरोजगार, किसी काम का नहीं आदि महसूस करतें है जिससे हम तनाव में रहतें हैं
Read More –
- अधिगम का अर्थ? प्रयास एंव त्रुटी सिद्धांत?
- अधिगम के सिद्धांत – सूझ एंव अनुबंधन का सिद्धांत?
- अनुभूति का गेस्टाल्ट सिद्धांत, प्रत्यक्षीकरण?
- इमोशन क्या है? संवेग या भावनाएं का अर्थ?
- जैविक, मनोगतिक, व्यवहारवादी और संज्ञानात्मक दृष्टिकोण?
- तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं?
- ध्यान क्या है? प्रकार, विशेषताएं?
- प्रेरणा का अर्थ, प्रकृति, प्रकार, विशेषताएं?
- बुद्धि क्या है? बुद्धि-लब्धि ( I.Q )
FAQ
एटीट्यूड का मतलब क्या है हिंदी में?
मनोवृत्ति ( Attitude ) शब्द लैटिन भाषा के Aptus शब्द से लिया गया हैं जिसका अर्थ योग्यता या सुविधा होता है मनोवृत्ति/अभिवृत्ति का अर्थ रवैया या दृष्टिकोण होता हैं इसीलिए मनोवृत्ति को अभिवृत्ति या दृष्टिकोण भी कहा जाता है
एटीट्यूड से आप क्या समझते हैं?
मनोवृत्ति ( Attitude ) का मतलब मनुष्य/व्यक्ति के उस दृष्टिकोण ( Drishtikon ) से होता हैं जिसके कारण वह व्यक्ति किन्ही परिस्थितियों, वस्तुओं, संस्थाओं, योजनाओं,
व्यक्तियों आदि के प्रति किसी विशेष प्रकार का व्यवहार करता है मनोवृत्ति के निर्माण में व्यवहार के प्रत्यक्षात्मक, प्रेरणात्मक, संवेगात्मक और क्रियात्मक पक्ष निहित रहते हैं
सकारात्मक मनोवृत्ति क्या है?
सकारात्मक मनोवृत्ति या एटीट्यूड के कारण आस-पास के लोग हमे अधिक महत्त्व देना पसंद करतें हैं क्योकि सकारात्मक एटीट्यूड हमारे भावनात्मक कल्याण और ख़ुशी को कई गुणा बढाने में हमारी मदद करता हैं
अगर आप किसी कार्य को सकारात्मक एटीट्यूड के साथ कर रहें है तब ऐसी स्थिति में आप उस कार्य को अपनी पुरी हिम्मत के साथ कार्य करके उसके सफलता प्राप्त करने की संभावना में वृद्धि करतें है
मनुष्य के व्यवहार में एटीट्यूड की क्या भूमिका है?
हर मनुष्य के लिए उसका एटीट्यूड उसकी पहचान बनता हैं क्योकि मनुष्य का एटीट्यूड उससे बातचीत करने वाले मनुष्यों को उसकी सोच, प्राथमिकता, कार्य को लेकर उत्त्सुकता, सफलता प्राप्त करने के लिए मजबूत निर्णय को दर्शाता हैं
उदहारण के लिए, जब हम किसी प्रोजेक्ट के लिए बोर्ड-मेम्बर के साथ मीटिंग में अपना पक्ष प्रेजेन्टेशन के साथ रखतें है तब उस दौरान हमारे एटीट्यूड पर अधिकतर बोर्ड-मेम्बर का फोकस रहता हैं
क्योकि अगर वह आपके प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के लिए दिलजस्पी रखते है तब यहाँ उनको आपके अंदर के एटीट्यूड को Observe करना होगा जिससे वह उस प्रोजेक्ट को लेकर आपके विचार, सोच, भविष्य प्लान, काबिलियत इत्यादि को सही जज कर सकें
मनोवृति कितने प्रकार की होती है?
मनोवृति कई प्रकार जैसे – मानसिक अभिवृत्ति, विशिष्ट अभिवृत्ति, सकरात्मक अभिवृत्ति, सामान्य अभिवृत्ति , नकारात्मक अभिवृत्ति |
मनोवृत्ति का निर्माण कैसे होता है?
मनोवृत्ति का निर्माण जन्मजात नहीं होती है बल्कि यह अर्जित की जाती हैं और यह अनुभवों के आधार पर अर्जित होती हैं तथा वस्तुओं, मूल्यों एंव व्यक्तियों के संबंध में सीखी जाती है
मनोवृति को कैसे बदला जा सकता है?
मनोवृत्ति परिवर्तन के लिए मनुष्य को सर्वप्रथम यह निर्णय लेना होगा कि वह सच में बदलना चाहता हैं उसके बाद अगर आप यह तय कर लेतें है कि आपको किस तरह अपना एटीट्यूड बदलना हैं
उसके बाद आपको अपना एटीट्यूड बदलने के लिए पहला प्रयास करना चाहिए हर व्यक्ति का एटीट्यूड धीरे-धीरे बदलता है उसके लिए हमे निरंतर खुद को Observe करते हुए प्रयास करतें रहना होता हैं
मनोवृत्ति कैसे एक व्यक्ति के लिए अहं रक्षात्मक कार्य करती है?
मनोवृत्ति कहानी को समझने वाले मनुष्यों को यह पता चल गया होगा कि इगो और एटीट्यूड एक नहीं हैं लेकिन अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रहता है तब वह आपके जीवन में खुद के अंदर इगो की मात्रा को बैलेंस करने का कार्य करता हैं
परन्तु जब व्यक्ति पॉजिटिव एटीट्यूड के कारण अपनी इगो की मात्रा बढाता हैं तब वह किये जाने वाले कार्य के लिए लापरवाह स्थिति पैदा करता है जो उस मनुष्य की असफलता का कारण बन जाती है इसीलिए कहा जाता है कि ओवर एटीट्यूड अच्छा नहीं होता है
मनोवृत्ति की क्या विशेषताएं हैं?
मनोवृति व्यवहार को प्रभावित करती हैं मतलब एक व्यक्ति की अभिवृत्तियों का प्रभाव दुसरे व्यक्ति की अभिवृत्ति पर पड़ता है मनोवृत्ति व्यक्ति के व्यवहार का प्रतिबिम्ब होती है
इसीलिए हम किसी मनुष्य के व्यवहार को देखकर उसकी अभिवृत्ति के बारे में पता कर सकतें है यह सदैव परिवर्तनशील होती हैं और यह सदैव संवेगों तथा भावों से प्रभावित होती हैं अभिवृत्ति का सम्बन्ध समस्याओं तथा आवश्यकताओं से होता है
निष्कर्ष
यह लेख विशेष रूप से इन्टरनेट सहित सोशल मीडिया की दुनिया में सबसे पोपुलर शब्द मनोवृत्ति ( Attitude ) को समझाने के उद्देश्य से शेयर किया गया हैं मनोवृत्ति क्या होती हैं? ( Manovriti Kya Hai ). को लेकर,
हमे यह समझना चाहिए कि मनोवृत्ति ( Attitude ) मनुष्य के व्यवहार को तय करता हैं क्योकि अगर आपको पता चलें कि किसी व्यक्ति ने आपका पैन चुरा लिया है तब आप उसको चोर की नजरों से देखतें हुए उसके प्रति अपने Attitude को गुस्से वाला रखेंगे
मैं यह उम्मीद करता हूँ कि कंटेंट में दी गई इनफार्मेशन आपको पसंद आई होगी अपनी प्रतिक्रिया को कमेंट का उपयोग करके शेयर करने में संकोच ना करें अपने फ्रिड्स को यह लेख अधिक से अधिक शेयर करें
लेखक – नितिन सोनी
नमस्ते! मैं एनएस न्यूज़ ब्लॉग पर एक राइटर के रूप में शुरू से काम कर रहा हूँ वर्तमान समय में मुझे पॉलिटिक्स, मनोविज्ञान, न्यूज़ आर्टिकल, एजुकेशन, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट जैसे अनेक विषयों की अच्छी जानकारी हैं जिसको मैं यहाँ स्वतंत्र रूप से शेयर करता रहता हूं मेरा लेख पढने के लिए धन्यवाद! प्रिय दुबारा जरुर आयें
