Attribution Meaning in Hindi: – गुणारोपण क्या है? सामान्यत: हम जब किसी मनुष्य से मिलतें हैं उसके द्वारा हमारे लिए किया गया व्यवहार हम दोनों के बीच होने वाले कम्युनिकेशन के लिए बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण होता है
अगर आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं ऐसी स्थिति में आपके प्रति उसका व्यवहार बुरा हैं तब ऐसी स्थिति आप उस मनुष्य के बुरे व्यवहार के कारणों और स्त्रोतों का पता लगाने का प्रयास करतें है यही गुणारोपण या आरोपण की प्रक्रिया होती है
मनोविज्ञान को पढने वाले स्टूडेंट के एग्जाम उद्देश्य से यह टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योकि अक्सर एग्जाम में आरोपण के विषय पर सवालों को देखा गया हैं इसीलिए मनोविज्ञान में आरोपण ( Attribution in Psychology ) को पढ़ना सरल बना दिया गया है

सबसे पहले हम एट्रीब्यूट ( Attribute ) के कुछ शाब्दिक अर्थों को समझतें हुए आरोपण किसे कहते हैं? ( Attribution Definition Psychology ) पर चर्चा करना शुरू कर देंगे
Attribute Meaning in Hindi – Meaning of Attribute in Hindi – Attribute Hindi Meaning.
एट्रीब्यूट ( Attribute ) का शाब्दिक अर्थ “गुण या विशेषता” होता हैं अन्य अर्थों में एट्रिब्यूट को गुण बताना, श्रेय देना, आरोपित करना, अनुमान लगाना, गुणवत्ता, ग्रन्थकारिता का अनुमान बताया जा सकता हैं
Attributing Meaning in Hindi – Attribution Meaning ( Meaning of Attribution ) Attribution Psychology.
आरोपण ( Attribution ) का सामान्य अर्थ अधिकार, श्रेय देना, आरोप, स्त्रोत को निर्दिष्ट करना या बताना, लगाव, सम्बन्ध, जिम्मेदार ठहराना इत्यादि को समझा जा सकता है उदहारण के लिए,
- उसने पेंटिंग के पिकासोसे सम्बंधित होने पर सवाल उठाया
- वह अपनी सफलता का श्रेय कड़ी मेहनत और थोड़ी सी किस्मत को देती हैं
Attribution Meaning in Hindi – Meaning of Attribution in Hindi – What is Attribution in Psychology – Define Attribution.
एट्रीब्यूशन की अवधारणा यह बताती है कि व्यक्ति अपने जीवन में होने वाली घटनाओं और व्यवहारों के कारणों का अनुमान कैसे लगातें है आमतौर पर बिना किसी जागरूकता के अपने वास्तविक जीवन में हम सभी हर दिन ऐसा करतें है
गुणारोपण एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक प्रक्रिया हैं जब भी कोई व्यक्ति किसी दुसरे व्यक्ति के व्यवहारों का प्रत्यक्षण करता है तो उस समय वह मात्र इतनी ही जानकारी से संतुष्ट नहीं हो जाता हैं कि उसने अमुक व्यवहार किया है
बल्कि वह उन व्यवहार के कारणों अथवा उनकी उत्पत्ति के स्त्रोतों या प्रेरकों का भी अनुमान कर लेता हैं किसी व्यक्ति और उसके कार्यों एंव व्यवहारों को प्रत्यक्षण करते समय इस प्रकार का अनुमान कर लेना ही गुणारोपण कहलाता है
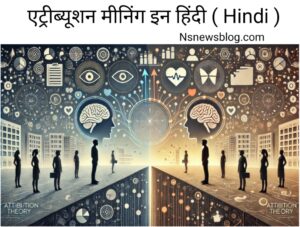
फेल्डमैन ( 1985 ) – दुसरे लोगो के व्यवहार के कारणों को समझना तथा उसके बारे में निर्णय लेना ही गुणारोपण कहा जाता है
बेरोन तथा बन ( 1987 ) – गुणारोपण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम लोग दूसरों के व्यवहारों के कारणों का निर्धारण करते है तथा उनके स्थायी शीलगुणों एंव चित-वृति के बारे में ज्ञान प्राप्त करतें है
साधारण भाषा – गुणारोपण की प्रक्रिया एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया हैं जिसके द्वारा दुसरे व्यक्तियों के व्यवहारों के कारण का पता चलता हैं प्रत्यक्षणकर्ता किसी लक्षित व्यक्ति के व्यवहारों का पहले प्रत्यक्षण करता हैं
उसके बाद उन व्यवहारों के संभावित कारणों को ढूढ़ता हैं और एक निश्चित निर्णय करता है
गुणारोपण की प्रक्रिया में लक्षित व्यक्ति के व्यवहार के पीछे छिपे कारणों पर बल ( Focus ) डाला जाता हैं और उसी के संदर्भ में उसके शीलगुणों एंव चित-वृति के बारे में किसी निर्णय पर पहुँचने की कोशिश की जाती हैं
उदहारण के लिए, मान लीजिए कोई महिला फटे-चिटे गंदे कपडें पहने हुए आप से भूकंप में गिरे घर की मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता मांगती हैं ऐसी परिस्थिति में आप मात्र उसकी शारीरिक स्थिति तथा फटे-चिटे कपडे के संदर्भ में ही,
उसके द्वारा किये गए आर्थिक सहायता की मांग का प्रत्यक्षण नहीं करते बल्कि यह भी अनुमान कर लेते है कि उसकी यह स्थिति वास्तविक ग़रीबी के कारण है या वह मात्र दूसरों को धोखा देकर पैसा कमाने के लिए भीख मांग रही है
गुणारोपण के आंतरिक तथा बाह्य कारक ( Internal & External Factors ).
गुणारोपण की प्रक्रिया को समान्यत: दो कारकों के रूप में समझने की कोशिश की गई हैं –
- आंतरिक कारक ( Internal Factor )
- बाह्य कारक ( External Factor )
आंतरिक कारक ( Internal Factor ) – इससे तात्पर्य उन कारकों से होता हैं जो लक्षित व्यक्ति जिसके व्यवहारों का कारण प्रत्यक्षणकर्ता ढूढता है उसमे निहित होते हैं इसमें मूल रूप से लक्षित व्यक्ति के योग्यता, शीलगुण आदि से सम्बंधित कारक होते हैं

बाह्य कारक ( External Factor ) – बाह्य कारक से तात्पर्य उन कारकों से होता है जो मूलतः वातावरण के कारकों से सम्बंधित होते है और उसी के रूप में लक्षित व्यक्ति के व्यवहारों के कारणों की व्याख्या की जाती हैं
उदहारण के लिए, मान लीजिए किसी कर्मचारी को नौकरी से निलंबित कर दिया जाता हैं इस निलंबन का कारण या तो कर्मचारी में ( आंतरिक कारक ) अथवा उसके बाहर ( बाह्य कारक ) या अंशत: दोनों में स्थित हो सकतें हैं
आंतरिक कारकों में कर्मचारी की बुरी लत, मानसिक अयोग्यता, काम में अरुचि आदि हो सकतें हैं तथा बाह्य कारकों में उसके बॉस की सख्त मनोवृति, कार्य का दुर्लभ स्वरूप, कार्य के वातावरण का असंतोषजनक होना आदि हो सकता है
कार्य-कारण का आरोपण – Attribution of Causality.
कार्य-कारण का आरोपण घटनाओं, व्यवहारों या परिणामों के कारणों को निर्धारित करने या समझाने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है इसमें उन कारकों या चर की पहचान करना शामिल है जो किसी विशेष परिणाम के लिए जिम्मेदार हैं

कार्य-कारण गुण मानवीय संज्ञान का एक मूलभूत पहलू है और दुनिया को समझने और हमारे अनुभवों को समझने के लिए आवश्यक है सिद्धांत है जो बतातें हैं कि लोग किस प्रकार कार्य-कारण को जिम्मेदार मानतें है
- फ्रिट्ज हेइडर एट्रीब्यूशन सिद्धांत ( Fritz Heider Attribution Theory )
- केली का आरोपण सिद्धांत ( Harold Kelly’s Attribution Theory )
- वेनर का आरोपण सिद्धांत ( Bernard Weiner’s Attribution Theory )
- जोन्स और डेविस का संवाददाता अनुमान सिद्धांत
फ्रिट्ज हेइडर एट्रीब्यूशन सिद्धांत ( Fritz Heider Attribution Theory ) – Attribution Theory in Social Psychology.
एट्रीब्यूशन थ्योरी का विकास फ्रिट्ज हेइडर ( Fritz Heider ) ने किया था उन्होंने इस अवधारणा को सबसे पहले सामाजिक मनोविज्ञान में पेश किया था यह एट्रीब्यूशन के सबसे प्रसिद्ध सिद्धनों में से एक हैं
जो आंतरिक ( व्यक्तिगत ) और बाह्य ( स्थितिजन्य ) एट्रीब्यूशन के बीच अंतर स्पष्ट करता है उन्होंने यह भी प्रस्तावित किया कि लोग दो प्रकार के एट्रीब्यूशन करतें है
- आंतरिक एट्रीब्यूशन ( Internal Attribution )
- बाह्य एट्रीब्यूशन ( External Attribution )
आंतरिक एट्रीब्यूशन ( Internal Attribution ) – यह किसी व्यक्ति की विशेषता या व्यक्तित्व के आधार पर किया गया आरोपण हैं मतलब आंतरिक आरोपण जब व्यक्ति किसी घटना या व्यवहार का कारण शामिल,
व्यक्ति की व्यक्तिगत विशेषताओं और स्वभाव को बताता हैं आंतरिक श्रेय में उसकी सफलता का श्रेय उसकी बुद्धिमता या प्रयास को देना शामिल हो सकता हैं
बाह्य एट्रीब्यूशन ( External Attribution ) – यह आस-पास की स्थिति या वातावरण के लिए किया गया आरोपण हैं मतलब बाहरी आरोप जब व्यक्ति किसी घटना या व्यवहार का कारण बाहरी कारकों या परिस्थितियों को बताता है
बाहरी श्रेय में व्यक्ति की सफलता का श्रेय एक आसान परीक्षा या सहायक शिक्षक को देना शामिल हो सकता है
हेरोल्ड केली का आरोपण सिद्धांत – Harold Kelly’s Attribution Theory ( Social Cognition Theory ).
सहपरिवर्तन सिद्धांत ( 1973 ) – इसे हेरोल्ड केली ( Harold Kelley ) द्वारा विकसित किया गया था इसको केली के कोवेरिएक्शन मॉडल के रूप में भी जाना जाता है यह एट्रीब्यूशन के क्षेत्र में एक व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त मॉडल है
यह बताता है कि मनुष्य किस तरह से कारण संबंधी निष्कर्ष निकालते है कि किसी व्यक्ति ने किसी ख़ास तरीकें से व्यवहार क्यों किया यह तीन मुख्य कारकों की जांच करके किया जाता है
- आम सहमति ( Consensus )
- संगति ( Consistency )
- विशिष्टता ( Distinctiveness )
आम सहमति ( Consensus ) – व्यक्ति यह देखता है कि अन्य लोग समान स्थिति में समान व्यवहार प्रदर्शित करतें है यदि किसी स्थिति में कई लोग एक जैसा व्यवहार करते है तो इसका कारण बाहरी कारकों को माना जा सकता है
उदहारण के लिए, आप अपने अन्य सहकर्मीयों से बात करतें हैं और पाते है कि उन्होंने भी देखा है कि आपका दोस्त अक्सर काम पर बुरे मूड में रहता है आपके मित्र के व्यवहार को लेकर आपके सहकर्मीयों के बीच आम सहमति हैं
दुसरा उदहारण – क्या अन्य लोग भी इस स्थिति में इसी तरह प्रतिक्रिया करते है?
संगति ( Consistency ) – लोग इस बात पर विचार करतें है कि क्या व्यवहार या घटना लगातार किसी विशेष कारण से जुडी हुई हैं यदि कोई व्यक्ति लगातार कोई व्यवहार प्रदर्शित करता है
तो इसके लिए किसी विशिष्ट/अंतनिर्हित कारण की जिम्मेदारी ठहराए जाने की अधिक संभावना है
उदहारण के लिए, आप देख सकतें है कि आपका मित्र न केवल आज बल्कि अधिकांश दिनों में काम के दौरान चिड़चिड़ा रहता है यह उच्च स्थिरता बताती है कि उनके ख़राब मूड का कोई अंतनिर्हित कारण हो सकता है न कि यह कोई आकस्मिक घटना है
दुसरा उदहारण – क्या व्यक्ति हर बार स्थिति उत्पन्न होने पर एक ही तरह से प्रतिक्रिया करता है?
विशिष्टता ( Distinctiveness ) – लोग यह आकलन करतें है कि व्यवहार स्थिति के लिए विशिष्ट हैं या नहीं यदि कोई व्यवहार किसी विशेष स्थिति के लिए अत्यधिक विशिष्ट हैं और अन्य स्थितियों में घटित नहीं होता है
तो व्यक्तियों द्वारा इसे बाहरी कारणों से जिम्मेदार ठहराने की अधिक संभावना होती है उदहारण के लिए, आप देखतें है कि आपका मित्र केवल काम पर क्रोधी हैं अन्य स्थानों पर नहीं जैसे कि जब आप काम के अलावा बाहर घूमते हैं
इस कम विशिष्टता का तात्पर्य है कि उनके ख़राब मूड का कारण सामान्य स्वभाव नहीं बल्कि कार्य वातावरण विशिष्ट हो सकता हैं
दुसरा उदहारण – क्या व्यक्ति अन्य परिस्थितियों में भी उसी प्रकार पहुंचता है?
बर्नार्ड वेनर का आरोपण सिद्धांत – Bernard Weiner’s Attribution Theory ( Attribution in Social Psychology )
बर्नार्ड वेनर का एट्रीब्यूशन सिद्धांत विशेष रूप से उपलब्धि और प्रदर्शन संदर्भो पर लागू होता है इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि व्यक्ति अपनी सफलताओं और असफलताओं का श्रेय कैसे देता हैं
वेनर का सिद्धांत मानता है कि लोग तीन प्राथमिक आयामों के आधार पर कारणात्मक आरोप लगातें हैं
नियंत्रण का स्थान ( Locus of Control ) – यह आयाम संदर्भित करता है कि क्या किसी घटना का कारण आंतरिक ( व्यक्तिगत ) कारकों या बाहरी ( स्थितिजन्य ) कारकों को माना जाता है उदहारण के लिए,
- आंतरिक गुण – छात्र सोचता है मुझे गणित की परीक्षा में सी ग्रेड मिला हैं क्योकि मैं गणित में अच्छा नहीं हूँ मैंने पर्याप्त मेहनत से पढाई नहीं की हैं
- बाहरी गुण – छात्र सोचता है मुझे गणित की परीक्षा में सी प्राप्त हुआ हैं क्योकि परीक्षा असाधारण रूप से कठिन थी और प्रश्न पेचीदा थे
स्थिरता ( Stability ) – यह आयाम इस बात से सम्बंधित है कि क्या कारण को स्थिर ( समय के साथ बने रहने की संभावना ) या अस्थिर ( परिवर्तन की संभावना ) के रूप में देखा जाता हैं उदहारण के लिए,
- स्थिर गुण – छात्र का मानना है कि उसके गणित कौशल की कमी एक स्थिर कारक हैं वह सोचता है कि मुझे हमेशा गणित में संघर्ष करना पड़ा हैं और मैं शायद ऐसा करना जारी रखूंगा
- अस्थिर गुण – छात्र परीक्षा में कठिनाई को एक अस्थिर कारक के रूप में देखता हैं वह सोचता है कि यह परीक्षा असामान्य रूप से कठिन थी लेकिन मैं भविष्य में सुधार कर सकता हूँ
नियंत्रणीयता ( Controllability ) – यह आयाम इस बात से सम्बंधित हैं कि क्या कारण को व्यक्ति के नियंत्रण में या उनके नियंत्रण से परे कुछ के रूप में देखा जाता हैं
- नियंत्रणीय गुण – छात्र मानता हैं कि उसके प्रयास की कमी एक कारक थी तो वह सोच सकता हैं कि मैंने उतना अध्ययन नहीं किया जितना मुझे करना चाहिए था और मैं अपनी अध्ययन आदतों में सुधार कर सकता हूँ
- अनियंत्रित विशेषता – छात्र परीक्षा में कठिनाई के लिए ग्रेड को जिम्मेदार मानता हैं तो वह सोच सकता हैं कि परीक्षा मेरे नियंत्रण से बाहर थी और मैं इसके बारे में बहुत कुछ नहीं कर सकता
वेनर के सिद्धांत को अक्सर शैक्षिक और उपलब्धि सेटिंग्स में लागू किया जाता हैं ताकि यह समझा जा सकें कि छात्र अपनी सफलताओं और विफलताओं को कैसे समझातें है
यदि वह सी ग्रेड का श्रेय प्रयास की कमी ( आंतरिक, अस्थिर, नियंत्रणीय ) को देता हैं तब वे भविष्य में कठिन अध्ययन करने के लिए प्रेरित हो सकता हैं लेकिन यदि वे इसे परीक्षा की कठिनाई ( बाहरी, स्थिर, अनियंत्रित ) के लिए जिम्मेदार मानता है
तो वे अपनी अध्ययन की आदतों को बदलने में कम रूचि महसूस कर सकता है
जोन्स और डेविस का संवाददाता अनुमान सिद्धांत ( Jones & Davi’s Correspondence Inference Theory ).
इसे एडवर्ड जोन्स ( Edward Jones ) और कीथ डेविस ( Keith Davis ) द्वारा विकसित किया गया था इसने यह सिद्धांत बनाया कि लोग दूसरों के व्यवहार को उनके व्यक्तित्व गुण के अनुसार देखतें है यह तीन कारकों के आधार पर किया जाता है
- व्यक्ति की पसंद की डिग्री – क्या व्यक्ति के पास अपने कार्य में कोई विकल्प हैं?
- व्यवहार की अपेक्षितता – क्या यह व्यवहार हमारे समाज में अपेक्षित एंव सामान्य हैं?
- इच्छित प्रभाव या परिणाम – किसी कार्य के पीछे व्यक्ति का इरादा क्या है?
एट्रीब्यूशन त्रुटियाँ ( Attribution Errors )
- मौलिक आरोपण त्रुटियाँ या पत्राचार पूर्वाग्रह – लोगो द्वारा सभी परिस्थितिजन्य कारणों पर विचार किए बिना आंतरिक रूप से आरोप लगाने की अधिक संभावना होती है जो मौजूदा होतें है और अत्यधिक प्रभावशाली होतें है
- अभिनेता-पर्यवेक्षक पूर्वाग्रह – अभिनेताओं द्वारा अपने व्यवहार के लिए बाह्य कारणों को जिम्मेदार ठहराने की प्रवृत्ति तथा पर्यवेक्षकों द्वारा दूसरों के व्यवहार के लिए आंतरिक कारणों को जिम्मेदार ठहराने की प्रवृत्ति.
- स्वार्थी पूर्वाग्रह – यह लोगो की प्रवृत्ति हैं कि वे सकारात्मक परिणामों के लिए आंतरिक कारणों को जिम्मेदार ठहरातें है जबकि नकारात्मक परिणामों के लिए बाहरी कारकों को जिम्मेदार ठहरातें है
Read More –
- अधिगम का अर्थ? प्रयास एंव त्रुटी सिद्धांत?
- अधिगम के सिद्धांत – सूझ एंव अनुबंधन का सिद्धांत?
- अनुभूति का गेस्टाल्ट सिद्धांत, प्रत्यक्षीकरण?
- इमोशन क्या है? संवेग या भावनाएं का अर्थ?
- जैविक, मनोगतिक, व्यवहारवादी और संज्ञानात्मक दृष्टिकोण?
- तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं?
- ध्यान क्या है? प्रकार, विशेषताएं?
- प्रेरणा का अर्थ, प्रकृति, प्रकार, विशेषताएं?
- बुद्धि क्या है? बुद्धि-लब्धि ( I.Q )
FAQ
अटरीब्यूट का मतलब क्या होता है?
अटरीब्यूट का मतलब गुण या विशेषता होता हैं अन्य अर्थों में एट्रिब्यूट को गुण बताना, श्रेय देना, आरोपित करना, अनुमान लगाना, गुणवत्ता, ग्रन्थकारिता का अनुमान बताया जा सकता हैं
गुणारोपण किसे कहतें है?
गुणारोपण एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक प्रक्रिया हैं जब भी कोई व्यक्ति किसी दुसरे व्यक्ति के व्यवहारों का प्रत्यक्षण करता है तो उस समय वह मात्र इतनी ही जानकारी से संतुष्ट नहीं हो जाता हैं कि उसने अमुक व्यवहार किया है
बल्कि वह उन व्यवहार के कारणों अथवा उनकी उत्पत्ति के स्त्रोतों या प्रेरकों का भी अनुमान कर लेता हैं किसी व्यक्ति और उसके कार्यों एंव व्यवहारों को प्रत्यक्षण करते समय इस प्रकार का अनुमान कर लेना ही गुणारोपण कहलाता है
एट्रीब्यूशन क्या है उदाहरण दो?
मान लीजिए कोई महिला फटे-चिटे गंदे कपडें पहने हुए आप से भूकंप में गिरे घर की मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता मांगती हैं ऐसी परिस्थिति में आप मात्र उसकी शारीरिक स्थिति तथा फटे-चिटे कपडे के संदर्भ में ही,
उसके द्वारा किये गए आर्थिक सहायता की मांग का प्रत्यक्षण नहीं करते बल्कि यह भी अनुमान कर लेते है कि उसकी यह स्थिति वास्तविक ग़रीबी के कारण है या वह मात्र दूसरों को धोखा देकर पैसा कमाने के लिए भीख मांग रही है
इसीलिए एट्रीब्यूशन की अवधारणा यह बताती है कि व्यक्ति अपने जीवन में होने वाली घटनाओं और व्यवहारों के कारणों का अनुमान कैसे लगातें है आमतौर पर बिना किसी जागरूकता के अपने वास्तविक जीवन में हम सभी हर दिन ऐसा करतें है
निष्कर्ष
यह लेख विशेष रूप आरोपण क्या हैं? के लिए शेयर किया गया हैं यहाँ आरोपण परिभाषा ( Attribution Definition ) को अच्छे से समझाया गया हैं मनोविज्ञान के क्षेत्र में आरोपण का अर्थ हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए
क्योकि आरोपण एक मानसिक प्रक्रिया हैं एग्जाम के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमारे लेखक नितिन सोनी जी ने यूजर को यह विषय सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया हैं
मैं यह उम्मीद करता हूँ कि कंटेंट में दी गई इनफार्मेशन आपको पसंद आई होगी अपनी प्रतिक्रिया को कमेंट का उपयोग करके शेयर करने में संकोच ना करें अपने फ्रिड्स को यह लेख अधिक से अधिक शेयर करें
लेखक – नितिन सोनी
नमस्ते! मैं एनएस न्यूज़ ब्लॉग पर एक राइटर के रूप में शुरू से काम कर रहा हूँ वर्तमान समय में मुझे पॉलिटिक्स, मनोविज्ञान, न्यूज़ आर्टिकल, एजुकेशन, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट जैसे अनेक विषयों की अच्छी जानकारी हैं जिसको मैं यहाँ स्वतंत्र रूप से शेयर करता रहता हूं मेरा लेख पढने के लिए धन्यवाद! प्रिय दुबारा जरुर आयें
