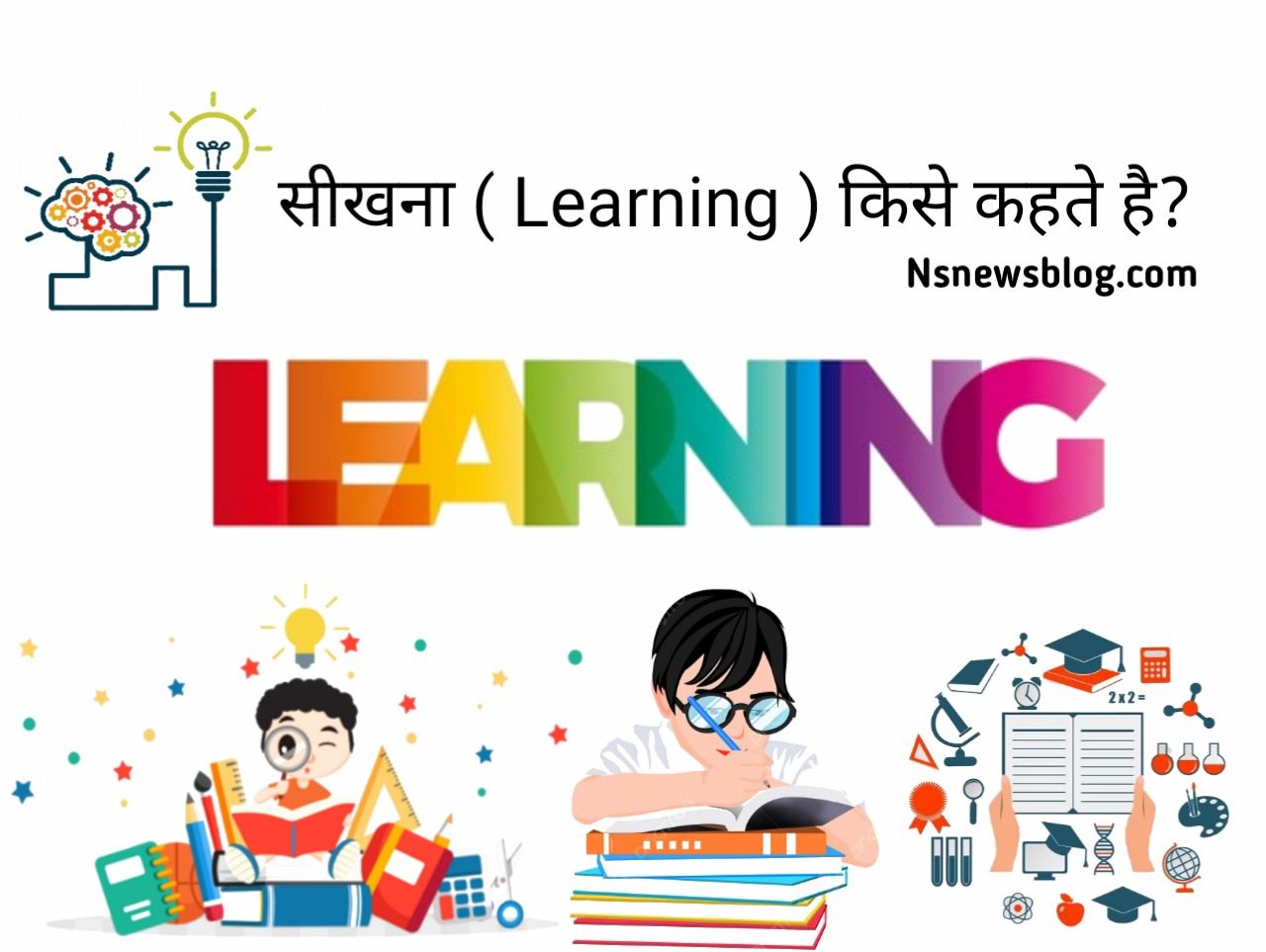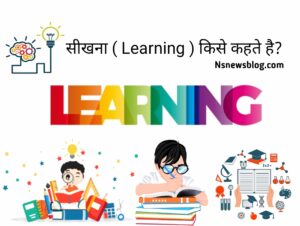Adhigam Kya Hai: – अधिगम का अर्थ या सीखने का अर्थ समझने के लिए आपको यह लेख अच्छे से पढ़ना होगा कुछ स्टूडेंट को अधिगम का दुसरा नाम नहीं पता होगा अधिगम को सीखना कहते हैं
सीखने का अर्थ एवं परिभाषा को एग्जाम में लिखने के लिए उसको इस लेख का उपयोग करके आपको समझना होगा सरल शब्दों में आप कह सकते हैं कि अधिगम वह प्रक्रिया है जिसमे किसी नई क्रिया का जन्म होता है
या सामने आयी हुई परिस्थिति के अनुकूल उसमे उचित परिवर्तन किया जाता हैं परन्तु अधिगम के सिद्धांत को मुख्य रूप से तीन भागों में रखा गया हैं जिसमें प्रयास एंव त्रुटी का सिद्धांत, सुझ और अनुबंधन का सिद्धांत शामिल हैं
प्रयास एंव त्रुटी के सिद्धांत में थार्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया जिसके माध्यम से थार्नडाइक ने भूखी बिल्ली को पिंजरे में लगा बटन दबाकर खाना सिखाया
हर मनुष्य जन्म के उपरांत सीखना प्रारंभ कर देता हैं और जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता हैं जिस मनुष्य में सीखने की शक्ति जितनी अधिक होती है उतना ही उसके जीवन का विकास होता है
इन्टरनेट पर बहुत अधिक मात्रा में लोगो के द्वारा कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि Adhigam Meaning in Hindi, अधिगम के प्रकार, Learn Meaning in Hindi, अधिगम का अर्थ और प्रकार, Meaning Of Learning in Hindi,
सीखने की प्रक्रिया क्या है, Learning Meaning in Hindi, अधिगम से क्या आशय है
चलिए अब हम यह समझ लेते है कि अधिगम क्या है? ( सीखना क्या है? )
Adhigam Kya Hai? ( अधिगम का अर्थ ) Learning in Hindi – Adhigam Meaning in Hindi – Meaning Of Learn in Hindi
अधिगम या सीखना वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमे व्यक्ति के स्वाभाविक व्यवहार में पूर्व अनुभव या प्रशिक्षण द्वारा परिवर्तन होता है पूर्व अनुभव या प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में होने वाला कोई भी परिवर्तन सीखना कहलाता हैं
मनोविज्ञान में सीखने से तात्पर्य केवल उन परिवर्तन से होता हैं जो अभ्यास या अनुभव के फलस्वरूप में होता हैं
पहला उदहारण, एक छोटे बच्चे के सामने जलती हुई मोमबत्ती को लाया जाए तो वह अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण उसको छुने के लिए दोड़ेगा परन्तु जब वह बच्चा उस जलती हुई मोमबत्ती को छु लेगा और वह जल जाएगा
परन्तु, इस स्थिति में उस बच्चे को एक अनुभव प्राप्त होगा जिसके कारण अगली बार वह बच्चा उस जलती हुई मोमबत्ती को छुने का प्रयास नहीं करेगा क्योकि ऐसा करने से उसको पता होगा कि वह जल जाएगा यहाँ बच्चे के स्वभाविक व्यवहार में परिवर्तन हुआ हैं
- अधिगम के सिद्धांत – सूझ एंव अनुबंधन का सिद्धांत?
- अनुभूति का गेस्टाल्ट सिद्धांत, प्रत्यक्षीकरण?
- अवलोकन क्या है? प्रयोगात्मक विधि?
- केस स्टडी का अर्थ और परिभाषा, गुण, दोष?
- जैविक, मनोगतिक, व्यवहारवादी और संज्ञानात्मक दृष्टिकोण?
दुसरा उदहारण, एक बच्चे को उसके पापा ने साइकिल गिफ्ट किया है परन्तु, अभी तक उस बच्चे के साइकिल को कभी नहीं चालाया हैं इसीलिए, वह बच्चा साइकिल चलाने के लिए ट्रेनिंग लेगा जिसके कारण, उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा
गेट्स तथा साथी – ने कहा कि सीखना अनुभव एंव प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार का परिमार्जन हैं
स्किनर – ने कहा कि सीखना व्यवहार के अर्जन में प्रगति की प्रक्रिया हैं
जे. पी. गिल्फार्ड – ने कहा कि हम इसकी परिभाषा व्यापक रूप में यह कहकर दे सकते हैं कि सीखना व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में कोई परिवर्तन!
कॉल्विन – ने कहा कि अनुभव के द्वारा पहले से बनाएं ( अथार्थ मौलिक ) व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम या सीखना कहलाता हैं
क्रो एंड क्रो – ने कहा कि सीखना, ज्ञान, आदतों और अभिवृत्तियों का अर्जन हैं
वुडवर्थ – ने कहा कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया हैं
क्राबैंक – अधिगम अनुभव के परिणामस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता हैं
ई. आर हिलगार्ड – अधिगम वह प्रक्रिया है जिसमे किसी नई क्रिया का जन्म होता है या सामने आयी हुई परिस्थिति के अनुकूल उसमे उचित परिवर्तन किया जाता हैं
- विस्मरण का अर्थ, कारण, महत्व, सिद्धांत?
- संवेदना का अर्थ और प्रत्यक्षीकरण क्या है?
- स्मृति का अर्थ, तत्व, परिभाषाएं, विशेषताएं?
अधिगम की विशेषताएँ ( सीखना की विशेषताएँ )
- अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है क्योकि सभी प्राणी में सीखने की प्रक्रिया होती हैं उदहारण, मनुष्य, जीव, पशु-पक्षी आदि
- सीखना जीवन-पर्यत चलने वाली प्रक्रिया हैं क्योकि व्यक्ति पुरे जीवन कुछ न कुछ सीखता रहता हैं
- यह एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया हैं क्योकि जब हम कोई चीज सीखते है तब हमारे व्यवहार, विचार, इच्छाएं और इमोशन में परिवर्तन होता हैं
- अधिगम की प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण होती हैं क्योकि बिना उद्देश्य के अधिगम संभव नहीं हैं जब हमारा कोई लक्ष्य होता है जिसको हमे प्राप्त करना होता है तब हम किसी कार्य को सीखने की शुरुआत करते हैं
- यह विकास की प्रक्रिया हैं क्योकि जब हम किसी कार्य को सीखते है तो हमारा शारीरिक और मानसिक विकास होता हैं
- सीखने की प्रक्रिया में समायोजन होता हैं क्योकि जब व्यक्ति किसी चीज को सीखता है तब उसे बहुत सारे समायोजन ( Adjustment ) करने पड़ते हैं यह समायोजन ( Adjustment ) वातावरण, परिस्थितियों के हिसाब से हो सकते हैं
- अधिगम में अनुभवों का संगठन होता हैं क्योकि जब मनुष्य कुछ सीखता हैं तब वह बहुत सारे लोगो, घटनाओं, वस्तुओं के संपर्क में आते हैं तब हमें इनके संपर्क में आने के कारण बहुत सारे अनुभव प्राप्त होते हैं
अपने इन अनुभवों को जब कोई व्यक्ति संगठित करता है तब वह बहुत सारी चीजों को सीख लेता हैं
- यह विवेकपूर्ण होता हैं क्योकि जब हम कोई चीज सीखते है तब हम यह समझ पाते है कि क्या सही है और क्या गलत हैं?
- सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया हैं जब हम किसी चीज को सीखते हैं तो हमे मानसिक और शारीरिक रूप से एक्टिव होना पड़ता हैं
- अधिगम की प्रक्रिया क्रमिक ( स्टेप बाई स्टेप ) होती हैं उदहारण, के लिए एक छोटा बच्चा पीठ के बल से, पेट के बल लेटना सीखेगा, जिसके बाद वह बैठने की क्रिया सीखेगा मतलब स्टेप बाई स्टेप होगी
- इसमें खोज होती हैं जब हम किसी चीज को सीखते है तब हम उसमे बहुत सारी नई नई चीजो को खोज सकते हैं
- सीखने की प्रक्रिया व्यक्तिगत भी होती हैं और सामाजिक होती हैं मतलब बहुत सारे ऐसे कार्य होते है जिनको व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से सीखता हैं और बहुत सारे कार्य या क्रिया ऐसी होती हैं जिनको मनुष्य समाज के संपर्क के द्वारा सीखता हैं
- अधिगम के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाये जा सकते हैं
अधिगम तथा परिपक्वता
परिपक्वता का संबंध शारीरिक-मानसिक शक्तियों के विकास से होता हैं एक नवजात शिशु ( मानव शिशु ) के जन्म के बाद से ही उसके शरीर का विकास होता है और जैसे जैसे विकास होता है तो उसके शरीर के विभिन्न अंगों में वृद्धि होती है,
वैसे – वैसे उन अंगों की शक्ति और क्षमता भी बढ़ती जाती हैं और विभिन्न अंगों की शक्ति और क्षमता का बढना और उनका सुदृढ होना ही परिपक्वता हैं
अधिगम और परिपक्वता में संबंध
परिपक्वता सीखने का आधार होता हैं क्योकि बिना परिपक्व ( Mature ) हुए, प्राणी चीजों को नहीं सीख सकता हैं, जब एक नवजात शिशु जन्म लेता हैं तब उसके शरीर में शक्ति का अभाव होता हैं परन्तु, जैसे जैसे उस बच्चे की आयु बढ़ती हैं
वैसे वैसे उसके शरीर में स्नायु मंडल का विकास होता है मतलब उसके शरीर की वृद्धि होती हैं जिससे उसके अंदर शारीरिक और मानसिक शक्ति में वृद्धि होती रहती हैं ठीक इसी तरह जब प्राणी बढ़ा होता है तब उसके सीखने की शक्ति में वृद्धि होती रहती हैं
इसीलिए परिपक्वता किसी व्यवहार को सीखने की एक आवश्यक शर्त हैं परिपक्वता के अभाव में प्राणी का सीखना असंभव हैं
उदहारण के लिए, एक छोटे बच्चे को आप जितना मर्जी चाहे साइकिल चालना सीखा लिजियें जब तक उसके हाथ, पैर परिपक्व ( Mature ) नहीं होंगे तब तक वह साइकिल चलाना नहीं सीखेगा
सीखना और परिपक्वता में अंतर
| सीखना ( अधिगम ) | परिपक्वता |
| सीखना एक अर्जित प्रक्रिया हैं क्योकि इसको प्राणी वातावरण के संपर्क में आकर सीखता हैं | जबकि परिपक्वता जन्मजात प्रक्रिया हैं क्योकि हर प्राणी में जन्म के बाद से, शारीरिक और मानसिक विकास का गुण होता हैं |
| विकास के क्रम में सीखने की प्रक्रिया परिपक्वता के बाद होती हैं | परन्तु, विकास के क्रम में परिपक्वता अधिगम ( सीखना ) से पूर्व की प्रक्रिया हैं |
| सीखने पर अभ्यास का प्रभाव पड़ता हैं क्योकि हम जितना अधिक अभ्यास करते है उतना अच्छे से सीखते हैं | लेकिन, परिपक्वता पर अभ्यास का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हैं मतलब परिपक्वता का अभ्यास से कोई लेना देना नहीं होता हैं क्योकि एक प्राणी एक ख़ास उम्र पर बोलना, चलना, उठना, बैठना शुरू कर देता हैं |
| अधिगम एक व्यक्तिगत प्रक्रिया हैं क्योकि कोई मनुष्य जितना चाहता है उतना सीखता है और हर मनुष्य अलग अलग चीजो को सीखता है | परन्तु, परिपक्वता का सम्बन्ध प्रजातीय गुण से होता है क्योकि एक ख़ास प्रजाति के सभी प्राणी, में परिपक्वता एक प्रकार की होती है |
| सीखने पर वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता हैं सकारात्मक वातावरण में सीखने की प्रक्रिया तीव्र गति से होगी और नकारात्मक वातावरण में सीखने की प्रक्रिया धीमी हो जायेगी | परिपक्वता पर वातावरण का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है क्योकि ऐसा नहीं है कि बहुत प्रदूषण, धुल वाला, ख़राब वातावरण में बच्चे की ग्रोथ पर फर्क पडेगा |
| सीखने ( अधिगम ) पर प्रेरणा का प्रभाव पड़ता हैं क्योकि प्रेरणा के कारण प्राणी तीव्र गति से सीखता है | परन्तु, परिपक्वता पर प्रेरणा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है |
| सीखना एक सचेतन प्रक्रिया हैं मतलब जब प्राणी सीखता है तब वह पुरी तरह से चेतन्य होकर सीखता हैं क्योकि उसको पता होता है कि वह सीख रहा हैं | लेकिन परिपक्वता एक अचेतन प्रक्रिया हैं मतलब इसमें प्राणी को पता भी नहीं चलता हैं और उसका शारीरिक और मानसिक विकास होता रहता हैं |
अधिगम या सीखने के सिद्धांत ( अधिगम के सिद्धांत का वर्गीकरण )
मुख्य रूप से सीखने ( अधिगम ) के तीन सिद्धांत हैं
- प्रयास एंव त्रुटी का सिद्धांत
- सूझ या अंतदृष्टि का सिद्धांत
- अनुबंधन का सिद्धांत
प्रयास एंव त्रुटी का सिद्धांत
प्रयास एंव त्रुटी के सिद्धांत का प्रतिपादन थार्नडाइक ( अमेरिका मनोवैज्ञानिक ) के द्वारा किया गया था जिसको प्रयत्न एंव भूल का सिद्धांत और उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत ( S-R Theory ) भी कहा जाता हैं मतलब यह बहु-अनुक्रिया का नियम हैं
जब कोई मनुष्य किसी कार्य को करता है तब वह एक बार में उसको नहीं सीखता है बल्कि उसको सीखने के लिए अनेक प्रयास करता हैं मनुष्य के द्वारा किये गए हर प्रयास में वह अनेक समस्या ( त्रुटियां ) या भूले करता है
परन्तु, मनुष्य के द्वारा किये गये हर अगले प्रयास में समस्या ( त्रुटियां ) या भूल की संख्या कम होती रहती हैं और एक समय बाद, एक ऐसी अवस्था आती है जब हम बिना त्रुटी किये, एक बार में सही क्रिया करने लगते हैं
इसी को प्रयत्न एंव भूल द्वारा सीखने का सिद्धांत कहा जाता है यह सिद्धांत थार्नडाइक के एक प्रयोग पर आधारित हैं जिसको बिल्ली पर किया था
थार्नडाइक का बिल्ली पर प्रयोग
थार्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली को एक पिंजरे में रख दिया और बाहर मछली का टुकड़ा रख दिया पिंजरे में एक बटन लगा था जिसको दबाने से पिंजरे का दरवाजा खुल जाता था भोजन को देखकर भूखी बिल्ली पिंजरे से बाहर निकलने के लिए उछल-कूद करने लगती हैं
कभी वह पिंजरे की सलाखों को दांत से काटती हैं, कभी पंजे से उसे खरोंचती हैं इस दौरान भूल से बिल्ली का पंजा बटन पर पड़ जाता हैं और पिंजरे का दरवाजा खुल जाता है बिल्ली बाहर आकर मछली प्राप्त कर लेती हैं
कुछ समय बाद, दुबारा यह प्रक्रिया दोहराई जाती हैं मतलब जब बिल्ली को भूख लगती है तब उसको पिंजरे में बंद कर दिया जाता हैं परन्तु, इस बार बिल्ली पहले की तुलना में जल्दी बाहर आकर मछली प्राप्त कर लेती हैं
क्योकि बिल्ली को यह पता लग जाता हैं कि पिंजरे के इस तरफ कुछ ऐसा है जिसकी वजह से पिंजरे का दरवाजा खुल जाता हैं थार्नडाइक के द्वारा हर अगले प्रयास में बिल्ली गलतियाँ कम करती है और उसके पिंजरे से बहार आने का समय कम होता जाता हैं
अंत में एक ऐसा प्रयास भी देखने को मिलता है जब बिल्ली बिना किसी गलती के बिल्ली सीधे बटन दबाकर पिंजरे से बाहर आ जाती हैं
प्रयास एंव त्रुटी द्वारा सीखने की अवस्थाएं ( सीखने की प्रक्रिया के चरण )
नवीन परिस्थिति – बिल्ली के सामने नयी स्थिति आयी थी क्योकि प्रयोग में बिल्ली एक पिंजरे में बंद थी और वह पिंजरा एक विशेष प्रकार का बटन दबाने पर खुलता था यह बिल्ली के लिए एक नई स्थिति थी
लक्ष्य – प्रयोग में बिल्ली के सामने मछली के टुकड़े के रूप में भोजन था जिसको प्राप्त करने के लिए मछली पिंजरे से बाहर निकलना सीख पायी इसीलिए यह उसका लक्ष्य था
प्रेरणा – क्योकि प्रयोग में बिल्ली भूखी थी उसके अंदर भूख प्रेरक था इसीलिए वह पिंजरे से बाहर आना सीख पायी
मानसिक स्थिति – बिल्ली उस पिंजरे से बाहर निकलने के लिए तैयार थी क्योकि उसकी मानसिक स्थिति ऐसी थी जिसके कारण वह बाहर आना चाहती थी हम कह सकते है कि बिल्ली मानसिक रूप से तैयार थी
अगर बिल्ली बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं होती अब वह कभी पिंजरे से बाहर निकलना नहीं सीख पाती
बाधाएं – जब बिल्ली उस मछली के टुकड़े को प्राप्त करना चाहती थी तब उसके मार्ग में बाधाएं यह थी कि वह पिंजरे के अंदर बंद थी जो कि विशेष प्रकार का बटन दबाने पर ही खुलता था
प्रयास – बिल्ली ने उस पिंजरे से बाहर निकलने के लिए अनेक प्रयास किये मतलब बिल्ली केवल एक प्रयास में उस पिजंरे से बाहर निकलना नहीं सीख पायी उसके लिए बिल्ली ने अनेक प्रयास किये जो गलत या त्रुटिपूर्ण थे
इन सभी त्रुटिपूर्ण प्रयास को कम करके बिल्ली धीरे धीरे बाहर आना सीख पायी
आकस्मिक सफलता – बिल्ली को पिंजरे से बाहर आने में अचानक से सफलता प्राप्त हो गई जब उसका पंजा उस विशेष बटन पर पड़ा जिसको दबाने से वह पिंजरा खुलता था ऐसा करने से उसको अचानक सफलता प्राप्त हो गई
जिसके बाद बिल्ली उस पिंजरे से बाहर आकर मछली प्राप्त कर लेती हैं
उचित समाधान – जब एक बार हमे सफलता प्राप्त हो जाती हैं तब हम उसी उचित समाधान का बार बार करते हैं
सफल चेष्टा का दोहराव – जो सफल प्रयास होता है जिसके कारण सफलता प्राप्त हुई हैं उस सफल प्रयास को बार बार दोहराना प्राणी शुरू कर देता हैं जिसके कारण गलत चेष्टा को मनुष्य छोड़ देता हैं
थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादन सीखने के नियम
थार्नडाइक के द्वारा सीखने का बनाया गया प्रयास एंव त्रुटी का सिद्धांत तीन मुख्य नियमों पर आधारित हैं
तत्परता या तैयारी का नियम – किसी भी कार्य को सीखने के लिए प्राणी का मानसिक रूप से तत्पर या तैयार होना आवश्यक हैं जब तक प्राणी सीखने के लिए स्वयं तैयार नहीं होगा तब तक वह किसी कार्य को नहीं सीख पाएगा
क्योकि जब कोई मनुष्य किसी कार्य को करने के लिए पहले से तैयार रहता हैं तो वह कार्य उसे आनंद देता हैं तथा आसानी और शीघ्रता से उस कार्य को सीख लेता है
परन्तु जब कोई मनुष्य किसी कार्य को करने के लिए तैयार नहीं रहता हैं या सीखने के लिए उसकी इच्छा नहीं होती है तो वह झुंझला जाता है या क्रोधित होता है जिसके कारण सीखने की गति धीमी हो जाती हैं या वह उस कार्य को नहीं सीख पाता हैं
अभ्यास का नियम – किसी कार्य को सीखने के लिए अभ्यास बहुत आवश्यक हैं जब हम किसी कार्य को बार बार दोहराते है तो हम उस कार्य को सीख जाते हैं परन्तु हम जिस कार्य ( क्रिया ) को छोड़ देते हैं या बहुत समय तक नहीं करते है
तब हम उसे भूलने लगते हैं इस नियम को उपयोग तथा अनुपयोग का नियम भी कहा जाता है जैसे – गणित के प्रश्न हल करना, टाइप करना, साइकिल चलाना आदि
उदहारण के लिए, एक छोटा बच्चा जब लिखना शुरू करता है तब शुरू में वह अक्षर सही से लिख नहीं पाते हैं परन्तु, लगातार अभ्यास करने पर वह सही तरीके से अक्षरों को लिखना सीख जातें हैं
प्रभाव का नियम – प्रभाव का अर्थ परिणाम से हैं यदि किसी कार्य को करने में हमे सफलता प्राप्त होती हैं या उसका परिणाम हमारे लिए सुखद व संतोषजनक होता है तो उस कार्य को हम बार बार करने लगते हैं
क्योकि उसका हमारे ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ता हैं इसके विपरीत जिस प्रयास से असफलता मिली हैं या जिसका परिणाम दुखद असंतोषजनक होता है उसे हम करना छोड़ देते हैं इस नियम को सुख तथा दुःख या पुरस्कार तथा दंड का नियम भी कहा जाता हैं
उदहारण के लिए, प्रयोग में बिल्ली पिंजरे से बाहर निकलने के लिए शुरू में उसको अपने दांत से काट रही थी, अपने पंजे से खरोंचने का प्रयास कर रही थी परन्तु, ऐसा करने से बिल्ली को कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई
इसीलिए, बिल्ली ने उन प्रयासों को करना छोड़ दिया बल्कि बिल्ली ने उस तरफ अपना प्रयास जारी रखा जिस तरह बटन लगा था
प्रयास एंव त्रुटी सिद्धांत का महत्त्व
शैक्षिक क्षेत्र व सामान्य जीवन में प्राय: सभी लोग अनेक कार्य प्रयास एंव त्रुटी ( भूल ) विधि के द्वारा सीखते है छोटे बच्चे व मंदबुद्धि बालक अधिकांश बातें व कार्य इसी विधि से सीखते हैं गणित तथा व्याकरण के क्षेत्र में यह विधि सबसे महत्त्वपूर्ण होती हैं
क्योकि गणित में हम प्रश्न का हल एक बार में नहीं निकाल पाते हैं परन्तु जब हम बार बार प्रयास करते है तब बिना गलती किये उन सवालों को आसानी से कर लेते है परन्तु, इस विधि का एक दोष मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बताया जाता है कि
यह विधि मुख्य रूप से पशुओं के सीखने की व्याख्या करती हैं मतलब मनुष्य के सीखने की व्याख्या या उस तरीके से नहीं कर पाती है क्योकि मनुष्य के सामने जब कोई नवीन परिस्थिति में आती हैं तब कुछ ऐसे प्रयास नहीं करता हैं
जैसे बिल्ली ने उस पिंजरे से बाहर निकलने के लिए छड को दांत से काटने का प्रयास किया था या अपने पंजे से खरोंचने का प्रयास किया यहाँ मनुष्य अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए उस समस्या को सुलझाने का प्रयास करता हैं
जो इस सिद्धांत में देखने को नहीं मिलता है लेकिन फिर भी यह सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है क्योकि यह सिद्धांत बच्चो के सीखने की व्याख्या बहुत अच्छे से करता है
Read More –
- इमोशन क्या है? संवेग या भावनाएं का अर्थ?
- तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं?
- ध्यान क्या है? प्रकार, विशेषताएं?
- प्रेरणा का अर्थ, प्रकृति, प्रकार, विशेषताएं?
- बुद्धि क्या है? बुद्धि-लब्धि ( I.Q )
- मनोविज्ञान ( Syllabus For Psychology )
- मनोविज्ञान क्या है? विकास, अर्थ, क्षेत्र एंव प्रकृति?
- मानव नेत्र की संरचना और कान?
- मानव विकास क्या है?
निष्कर्ष
यह लेख सीखने के विषय का पहला भाग हैं जिसमे सीखने के अर्थ को परिभाषित करते हुए कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा सीखने की परिभाषा को बताया गया है जो स्टूडेंट के लिए एग्जाम के उद्देश्य से बहुत महत्वपूर्ण हैं
सीखने के प्रयास एंव त्रुटी सिद्धांत को सरल भाषा में समझाते हए थार्नडाइक के द्वारा सीखने के प्रयास एंव त्रुटी सिद्धांत में भूखी बिल्ली के प्रयोग के बारे में इनफार्मेशन दिया हैं
मैं यह उम्मीद करता हूँ कि कंटेंट में दी गई इनफार्मेशन आपको पसंद आई होगी अपनी प्रतिक्रिया को कमेंट का उपयोग करके शेयर करने में संकोच ना करें अपने फ्रिड्स को यह लेख अधिक से अधिक शेयर करें
लेखक – नितिन सोनी